देश के पर्यावरण और जल-संसाधनों पर जीवन भर महत्वपूर्ण कार्य करने वाले स्व. अनुपम मिश्र के बड़े सरोकारों में अपने समाज की भाषा बहुत ऊपर रहती थी.
उनका एक पुराना लेख -
भाषा
और पर्यावरण
- अनुपम मिश्र
किसी
समाज का पर्यावरण पहले बिगड़ना शुरू होता है या उसकी भाषा? हम इसे समझ कर संभल सकने के दौर से तो अभी आगे बढ़ गए हैं. हम विकसित हो
गए हैं.
भाषा
यानी केवल जीभ नहीं. भाषा यानी मन और माथा भी. एक का नहीं, एक बड़े समुदाय का मन और माथा, जो अपने आस–पास के और दूर के भी संसार को देखने–परखने–बरतने का संस्कार अपने में सहज संजो लेता है. ये संस्कार बहुत कुछ उस समाज
के मिट्टी, पानी, हवा में अंकुरित होते
हैं, पलते–बढ़ते हैं और यदि उन में से
कुछ मुरझाते भी हैं तो उनकी सूखी पत्तियां वहीं गिरती हैं, उसी
मिट्टी में खाद बनाती हैं. इस खाद यानी असफलता की ठोकरों के अनुभव से भी समाज नया
कुछ सीखता है.
लेकिन
कभी–कभी समाज के कुछ लोगों का माथा थोड़ा बदलने लगता है. यह माथा फिर अपनी
भाषा भी बदलता है. यह सब इतने चुपचाप होता है कि समाज के सजग माने गए लोगों के भी
कान खड़े नहीं हो पाते. इसका विश्लेषण, इसकी आलोचना तो दूर,
इसे कोई क्लर्क या मुंशी की तरह भी दर्ज नहीं कर पाता.
इस
बदले हुए माथे के कारण हिंदी भाषा में ५०–६० बरस में
नए शब्दों की एक पूरी बारात आई है. बरातिये एक से एक हैं पर पहले तो दूल्हे राजा
को ही देखें. दूल्हा है विकास नामक शब्द. ठीक इतिहास तो नहीं मालूम है कि यह शब्द
हिंदी में कब पहली बार आज के अर्थ में शामिल हुआ होगा. पर जितना अनर्थ इस शब्द ने
पर्यावरण के साथ किया है, उतना शायद ही किसी और शब्द ने
पर्यावरण के साथ किया हो.
विकास
शब्द ने माथा बदला और फिर उसने समाज के अनगिनत अंगो की थिरकन को थामा. अंग्रेजों
के आने से ठीक पहले तक समाज के जिन अंगों के बाकायदा राज थे, वे लोग इस भिन्न विकास की अवधारणा के कारण आदिवासी कहलाने लगे. नए माथे ने
देश के विकास का जो नया नक्शा बनाया, उसमें ऐसे ज्यादतर
इलाके पिछड़े शब्द के रंग से ऐसे रंगे गए, जो कई पंचवर्षिय
योजनाओं के झाड़ू–पोंछे से भी हल्के नहीं पड़ पा रहे. अब यह
हम भूल भी चुके हैं कि ऐसे ही पिछड़े इलाकों की संपन्नता से, वनों से, खनिजों, लौह–अयस्क से देश के अगुआ मान लिए गए हिस्से कुछ टिके से दिखते हैं.
कुछ
मुट्ठी भर लोग पूरे देश की देह का, उसके हर अंग
का विकास करने में जुट गए हैं. ग्राम विकास तो ठीक, बाल
विकास, महिला विकास सब कुछ लाईन में है.
अपने
को,
अपने समाज को समझे बिना उसके विकास की इस विचित्र उतावली में गजब की
सर्वसम्मति है. सभी राजनैतिक दल, सभी सरकारें फिर चाहे वे
मिशन वाली हो या वर्ग संघर्ष वाली, गर्व से विकास के काम में
लगी हैं. विकास की इस नई अमीर भाषा ने एक नई रेखा भी खींची है – गरीबी की रेखा. लेकिन इस रेखा को खींचने वाले संम्पन्न लोगों की गरीबी तो
देखिए कि उनकी तमाम कोशिशें रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या में कमी लाने के
बदले उसे लगातार बढ़ाती जा रही हैं.
पर्यावरण
की भाषा इस सामाजिक–राजनीतिक भाषा से रत्ती–भर अलग नहीं है. वह हिंदी भी है यह कहते हुए डर लगता है. बहुत हुआ तो आज
के पर्यावरण की ज्यादातर भाषा देवनागरी कही जा सकती है. लिपि के कारण राजधानी में
पर्यावरण मंत्रालय से लेकर हिंदी राज्यों के कस्बों, गांवों
तक के लिए बनी पर्यावरण संस्थाओं की भाषा कभी पढ़ कर तो देखें. ऐसा पूरा साहित्य,
लेखन, रिपोर्ट सबकुछ एक अटपटी हिंदी से पटा
पड़ा है.
कचरा
शब्दों का और उन से बनी विचित्र योजनाओं का ढेर लगा है. इस ढेर को पुनर्चक्रित भी
नहीं किया जा सकता. दो–चार नमूने देखें. सन् १९८० से
आठ–दस बरस तक पूरे देश में सामाजिक वानिकी नामक योजना चली.
किसी ने भी नहीं पूछा कि पहले यह तो बता दो कि असामाजिक वानिकी क्या है? यदि इस शब्द का, योजना का संबंध समाज के वन से है,
गांव के वन से है, तो हर राज्य के गांवों में
ऐसे विशिष्ट ग्रामवन, पंचायती वनों के लिए एक भरा पूरा शब्द
भंडार, विचार और व्यवहार का संगठन काफी समय तक रहा है.
कहीं
उस पर थोड़ी धूल चढ़ गई थी तो कहीं वह मुरझा गया था, पर
वह मरा तो नहीं था. उस दौर में कोई संस्था आगे नहीं आई इन बातों को लेकर. मरु
प्रदेश में आज भी मौजूद हैं ओरण, एक शब्द जो ‘अरण्य‘ से बना है. ये गांवों के वन, मंदिर, देवी के नाम पर छोड़े जाते हैं. कहीं कहीं तो
मीलों फैले हैं ऐसे जंगल. इनके विस्तार की, संख्या की कोई
व्यवस्थित जानकारी नहीं है. वन विभाग कल्पना भी नहीं कर सकता कि लोग ओरणों से एक
तिनका भी नहीं उठाते.
अकाल
के समय में ही इनको खोला जाता है. वैसे ये खुले ही रहते हैं, न कटीले तारों का घेरा है, न दीवारबंदी ही. श्रद्धा,
विश्वास का घेरा इन वनों की रखवाली करता रहा है. हजार–बारह सौ बरस पुराने ओरण भी यहां मिल जाएंगे. जिसे कहते हैं बच्चे–बच्चे की जबान पर ओरण शब्द रहा है. पर राजस्थान में अभी कुछ ही बरस पहले
तक सामाजिक संस्थाएं ही नहीं, श्रेष्ठ वन विशेषज्ञ भी या तो
इस परंपरा से अपरिचित थे या अगर जानते थे तो कुछ कुतुहल भरे, शोध वाले अंदाज में. ममत्व नहीं था, यह हमारी परंपरा
है ऐसा भाव नहीं था उस जानकारी में.
ऐसी
हिंदी की सूची लंबी है, शर्मनाक है. एक योजना देश की
बंजर भूमि के विकास की आई थी. उसकी सारी भाषा बंजर ही थी. सरकार ने कोई ३०० करोड़
रुपया लगाया होगा पर यह भूमि बंजर की बंजर ही रही. फिर योजना ही समेट ली गई. और अब
सबसे ताजी योजना है जलागम क्षेत्र विकास की. यह अंग्रेजी के वॉटरशेड डेवलपमेंट का
हिन्दी अनुवाद है. इससे जिनको लाभ मिलेगा, वे लाभार्थि
कहलाते हैं, कहीं हितग्राही भी हैं.
‘यूजर्स ग्रुप‘ का सीधा अनुवाद उपयोगकर्ता समूह भी
यहां है. तो एक तरफ साधन संम्पन्न योजनाएं हैं, लेकिन समाज
से कटी हुई. जन भागीदारी का दावा करती हैं पर जन इससे भागते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ मिट्टी और पानी के खेल को कुछ हजार बरस से समझने वाला समाज
है. उसने इस खेल में शामिल होने के लिए कुछ आनंददायी नियम, परंपराएं
और संस्थाएं बनाई थीं. किसी अपरिचित शब्दावली के बदले एक बिल्कुल आत्मीय ढांचा
खड़ा किया था. चेरापूंजी, जहां पानी कुछ गज भर गिरता है,
वहां से लेकर जैसलमेर तक जहां कुल पांच–आठ इंच
वर्षा हो जाए तो भी आनंद बरस गया– ऐसा वातावरण बनाया.
हिमपात
से लेकर रेतीली आंधी में पानी का काम, तालाब में
काम करने वाले गजधरों का कितना बड़ा संगठन खड़ा किया गया होगा. कोई चार–पाँच लाख गांवों में काम करने वाले उस संगठन का आकार इतना बड़ा था कि वह
सचमुच निराकार हो गया. आज पानी का, पर्यावरण का काम करने
वाली बड़ी से बड़ी संस्थाएं उस संगठन की कल्पना तो करके देखें. लेकिन वॉटरशेड,
जलागम क्षेत्र विकास का काम कर रही संस्थाएं, सरकारें,
उस निराकार संगठन को देख ही नहीं पातीं. उस संगठन के लिए तालाब एक
वॉटर बॉडी नहीं था. वह उसकी रतन तलाई थी. झुमरी तलैया थी, जिसकी
लहरों में वह अपने पुरखों की छवि देखता था. लेकिन आज की भाषा जलागम क्षेत्र को
मत्स्य पालन से होने वाली आमदनी में बदलती है.
इसी
तरह अब नदियां यदि घर में बिजली का बल्ब न जला पाएं तो माना जाता है कि वे “व्यर्थ में पानी समुद्र में बहा रही हैं“. बिजली
जरूर बने, पर समुद्र में पानी बहाना भी नदी का एक बड़ा काम
है. इसे हमारी नई भाषा भूल रही है. जब समुद्रतटीय क्षेत्रों में भूजल बड़े पैमाने
पर खारा होने लगेगा तब हमें नदी की इस भूमिका का पता चलेगा.
लेकिन
आज तो हमारी भाषा ही खारी हो चली है. जिन सरल, सजल शब्दों
की धाराओं से वह मीठी बनती थी उन धाराओं को बिल्कुल नीरस, बनावटी,
पर्यावरणीय, परिस्थितिक जैसे शब्दों से बाँधा
जा रहा है. अपनी भाषा, अपने ही आंगन में विस्थापित हो रही है.
वह अपने ही आंगन में पराई बन रही है.
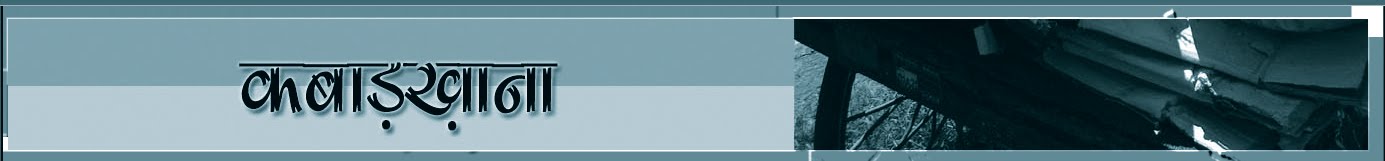

No comments:
Post a Comment