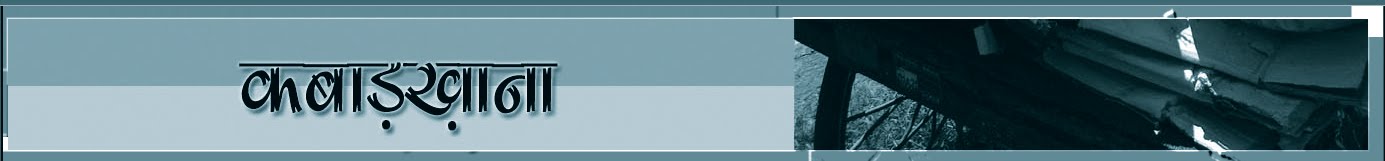'मां' जैसी क्लासिक रचना लिखने वाले महान रूसी साहित्यकार मैक्सिम गोर्की आज से क़रीब सौ साल पहले अमरीका गए थे पार्टी के लिए धन इकठ्ठा करने और समाजवाद के प्रचार हेतु। उनके तब के लिखे लिखे लेख एक पुस्तक की सूरत में सामने आए।
'मां' जैसी क्लासिक रचना लिखने वाले महान रूसी साहित्यकार मैक्सिम गोर्की आज से क़रीब सौ साल पहले अमरीका गए थे पार्टी के लिए धन इकठ्ठा करने और समाजवाद के प्रचार हेतु। उनके तब के लिखे लिखे लेख एक पुस्तक की सूरत में सामने आए।
पेश है उसी ज़रूरी किताब के एक अध्याय का पहला भाग। गणतन्त्र का एक सम्राट… संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्पात और तेल के सम्राटों और बाकी सम्राटों ने मेरी कल्पना को हमेशा तंग किया है। मैं कल्पना ही नहीं कर सकता कि इतने सारे पैसेवाले लोग सामान्य नश्वर मनुष्य हो सकते हैं।
मुझे हमेशा लगता रहा है कि उनमें से हर किसी के पास कम सप कम तीन पेट और डेढ़ सौ दांत होते होंगे। मुझे यकीन था कि हर करोड़पति सुबह छ: बजे से आधी रात तक खाना खाता रहता होगा। यह भी कि वह सबसे महंगे भोजन भकोसता होगा : बत्तखें¸ टर्की¸ नन्हे सूअर¸ मक्खन के साथ गाजर¸मिठाइयां¸ केक और तमाम तरह के लजीज व्यंजन। शाम तक उसके जबड़े इतना थक जाते होंगे कि वह अपने नीग्रो नौकरों को आदेश देता होगा कि वे उसके लिए खाना चबाएं ताकि वह आसानी से उसे निगल सके। आखिरकार जब वह बुरी तरह थक चुकता होगा¸ पसीने से नहाया हुआ¸ उसके नौकर उसे बिस्तर तक लाद कर ले जाते होंगे। और अगली सुबह वह छ: बजे जागता होगा अपनी श्रमसाध्य दिनचर्या को दुबारा शुरू करने को।
लेकिन इतनी जबरदस्त मेहनत के बावजूद वह अपनी दौलत पर मिलने वाले ब्याज का आधा भी खर्च नहीं कर पाता होगा।
निश्चित ही यह एक मुश्किल जीवन होता होगा। लेकिन किया भी क्या जा सकता होगा? करोड़पति होने का फायदा ही क्या अगर आप और लोगों से ज्यादा खाना न खा सकें?
मुझे लगता था कि उसके अंतर्वस्त्र बेहतरीन कशीदाकारी से बने होते होंगे¸ उसके जूतों के तलुवों पर सोने की कीलें ठुकी होती होंगी और हैट की जगह वह हीरों से बनी कोई टोपी पहनता होगा। उसकी जैकेट सबसे महंगी मलमल की बनी होती होगी। वह कम से कम पचास मीटर लम्बी होती होगी और उस पर सोने के कम से कम तीन सौ बटन लगे होते होंगे। छुट्टियों में वह एक के ऊपर एक आठ जैकेटें और छ: पतलूनें पहनता होगा। यह सच है कि ऐसा करना अटपटा होने के साथ साथ असुविधापूर्ण भी होता होगा … लेकिन एक करोड़पति जो इतना रईस हो बाकी लोगों जैसे कपड़े कैसे पहन सकता है …
करोड़पति की जेबें उस गडढे जैसी होती होंगी जिनमें वह समूचा चर्च¸ सीनेट की इमारत और छोटी मोटी जरूरतों को रख सकता होगा … लेकिन जहां एक तरफ मैं सोचता था कि इन महाशय के पेट की क्षमता किसी बड़े समुद्री जहाज के गोदाम जितनी होती होगी मुझे इन साहब की टांगों पर फिट आने वाली पतलून के आकार की कल्पना करने में थोड़ी हैरानी हुई। अलबत्ता मुझे यकीन था कि वह एक वर्ग मील से कम आकार की रजाई के नीचे नहीं सोता होगा। और अगर वह तम्बाकू चबाता होगा तो सबसे नफीस किस्म का और एक बार में एक या दो पाउण्ड से कम नहीं। अगर वह नसवार सूंघता होगा तो एक बार में एक पाउण्ड से कम नहीं। पैसा अपने आप को खर्च करना चाहता है …
उसकी उंगलियां अद्भुत तरीके से संवेदनशील होती होंगी और उनमें अपनी इच्छानुसार लम्बा हो जाने की जादुई ताकत होती होगी : मिसाल के तौर पर वह साइबेरिया में अंकुरित हो रहे एक डालर पर न्यूयार्क से निगाह में रख सकता था। अपनी सीट सेे हिले बिना वह बेरिंग स्टेट तक अपना हाथ बढ़ाकर अपना पसंदीदा फूल तोड़ सकता था।
अटपटी बात यह है कि इस सब के बावजूद मैं इस बात की कल्पना नहीं कर पाया कि इस दैत्य का सिर कैसा होता होगा। इसके अलावा मुझे लगा कि वह सिर मांसपेशियों और हडि्डयों का ऐसा पिण्ड होता होगा जिसकी गति को फकत हर एक चीज से सोना चूस लेने की इच्छा से प्रेरणा मिलती होगी। लब्बोलुबाब यह है कि करोड़पति की मेरी छवि एक हद तक अस्पष्ट थी। संक्षेप में कहूं तो सबसे पहले मुझे दो लम्बी लचीली बांहें नजर आती थीं। उन्होंने ग्लोब को अपनी लपेट में ले रखा था और उसे अपने मुंह की भूखी गुफा के पास खींच रखा था जो हमारी धरती को चूसता चबाता जा रहा था : उसकी लालचभरी लार उसके ऊपर टपक रही थी जैसे वह तन्दूर में सिंका कोई स्वादिष्ट आलू हो …
आप मेरे आश्चर्य की कल्पना कर सकते हैं जब एक करोड़पति से मिलने पर मैंने उसे एक निहायत साधारण आदमी पाया।
एक गहरी आरामकुर्सी पर मेरे सामने एक बूढ़ा सिकुड़ा सा शख्स बैठा हुआ था जिसके झुरीर्दार भूरे हाथ शान्तिपूर्वक उसकी तोंद पर धरे हुए थे। उसके थुलथुल गालों पर करीने से हजामत बनाई गई थी और उसका ढुलका हुआ निचला होंठ बढ़िया बनी हुई उसकी बत्तीसी दिखला रहा था जिसमें कुछेक दांत सोने के थे। उसका रक्तहीन और पतला ऊपरी होंठ उसके दांतों से चिपका हुआ था और जब वह बोलता था उस ऊपरी होंठ में जरा भी गति नहीं होती थी। उसकी बेरंग आंखों के ऊपर भौंहें बिल्कुल नहीं थीं और सूरज में तपा हुए उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। उसे देख कर महसूस होता था कि उसके चेहरे पर थोड़ी और त्वचा होती तो शायद बेहतर होता ; लाली लिए हुए¸ गतिहीन और मुलायम वह चेहरा किसी नवजात शिशु के जैसा लगता था। यह तय कर पाना मुश्किल था कि यह प्राणी दुनिया में अभी अभी आया है या यहां से जाने की तैयारी में है …
उसकी पोशाक भी किसी साधारण आदमी की ही जैसी थी। उसका धारण किया हुआ सोना घड़ी अंगूठी और दांतों तक सीमित था। कुल मिलाकर शायद वह आधे पाउण्ड से कम था। आम तौर पर वह यूरोप के किसी कुलीन घर के पुराने नौकर जैसा नजर आ रहा था …
जिस कमरे में वह मुझसे मिला उसमें सुविधा या सुन्दरता के लिहाज से कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। फ़र्नीचर विशालकाय था पर बस इतना ही था।
उसके फ़र्नीचर को देखकर लगता था कि कभी कभी हाथी उसके घर तशरीफ लाया करते थे।
"क्या आप … आप … ही करोड़पति हैं?" अपनी आंखों पर अविश्वास करते हुए मैंने पूछा।
" हां हां!" उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया।
मैंने उसकी बात पर विश्वास करने का नाटक किया और फैसला किया कि उसकी गप्प का उसी वक्त इम्तहान ले लूं।
"आप नाश्ते में कितना बीफ़ खा सकते हैं ?" मैंने पूछा।
"मैं बीफ़ नहीं खाता" उसने घोषणा की "बस सन्तरे की एक फांक एक अण्डा और चाय का छोटा प्याला …"
बच्चों जैसी उसकी आंखों में धुंधलाए पानी की दो बड़ी बूंदों जैसी चमक आई और मैं उनमें झूठ का नामोनिशान नहीं देख पा रहा था।
"चलिए ठीक है" मैंने संशयपूर्वक बोलना शुरू किया "मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे ईमानदारी से बताइए कि आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं ?"
"दिन में दो बार" उसने ठण्डे स्वर में कहा "नाश्ता और रात का खाना। मेरे लिए पर्याप्त होता है। रात को खाने में मैं थोड़ा सूप थोड़ा चिकन और कुछ मीठा लेता हूं। कोई फल। एक कप काफी। एक सिगार …"
मेरा आश्चर्य कद्दू की तरह बढ़ रहा था। उसने मुझे सन्तों की सी निगाह से देखा। मैं सांस लेने को ठहरा और फिर पूछना शुरू किया:
" लेकिन अगर यह सच है तो आप अपने पैसे का क्या करते हैं ?"
उसने अपने कन्धों को जरा उचकाया और उसकी आंखें अपने गड्ढों में कुछ देर लुढ़कीं और उसने जवाब दिया:
"मैं उसका इस्तेमाल और पैसा बनाने में करता हूं …"
"किस लिए ?"
"ताकि मैं और अधिक पैसा बना सकूं …"
"लेकिन किस लिए ?" मैंने हठपूर्वक पूछा।
वह आगे की तरफ झुका और अपनी कोहनियों को कुर्सी के हत्थे पर टिकाते हुए तनिक उत्सुकता से पूछा:
"क्या आप पागल हैं ?"
"क्या आप पागल हैं ?" मैंने पलट कर जवाब दिया।
बूढ़े ने अपना सिर झुकाया और सोने के दांतों के बीच से धीरे धीरे बोलना शुरू किया :
"तुम बड़े दिलचस्प आदमी हो … मुझे याद नहीं पड़ता मैं कभी तुम्हारे जैसे आदमी से मिला हूं …"
उसने अपना सिर उठाया और अपने मुंह को करीब करीब कानों तक फैलाकर खामोशी के साथ मेरा मुआयना करना शुरू किया। उसके शान्त व्यवहार को देख कर लगता था कि स्पष्टत: वह अपने आप को सामान्य आदमी समझता था। मैंने उसकी टाई पर लगी एक पिन पर जड़े छोटे से हीरे को देखा। अगर वह हीरा जूते ही एड़ी जितना बड़ा होता तो मैं शायद जान सकता था कि मैं कहां बैठा हूं।
"और अपने खुद के साथ आप क्या करते हैं?"
"मैं पैसा बनाता हूं।" अपने कन्धों के तनिक फैलाते हुए उसने जवाब दिया।
"यानी आप नकली नोटों का धन्धा करते हैं" मैं खुश होकर बोला मानो मैं रहस्य पर से परदा उठाने ही वाला हूं। लेकिन इस मौके पर उसे हिचकियां आनी शुरू हो गईं। उसकी सारी देह हिलने लगी जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे गुदगुदी कर रहा हो। वह अपनी आंखों को तेज तेज झपकाने लगा।
"यह तो मसखरापन है" ठण्डा पड़ते हुए उसने कहा और मेरी तरफ एक गीली संतुष्ट निगाह डाली। "मेहरबानी कर के मुझसे कोई और बात पूछिए" उसने निमंत्रित करते हुए कहा और किसी वजह से अपने गालों को जरा सा फुलाया।
मैंने एक पल को सोचा और निश्चित आवाज में पूछा:
"और आप पैसा कैसे बनाते हैं?"
"अरे हां! ये ठीकठाक बात हुई!" उसने सहमति में सिर हिलाया। "बड़ी साधारण सी बात है। मैं रेलवे का मालिक हूं। किसान माल पैदा करते हैं। मैं उनका माल बाजार में पहुंचाता हूं। आप को बस इस बात का हिसाब लगाना होता है कि आप किसान के वास्ते बस इतना पैसा छोड़ें कि वह भूख से न मर जाए और आपके लिए काम करता रहे। बाकी का पैसा मैं किराए के तौर पर अपनी जेब में डाल लेता हूं। बस इतनी सी बात है।"
"और क्या किसान इस से संतुष्ट रहते हैं?"
"मेरे ख्याल से सारे नहीं रहते!" बालसुलभ साधारणता के साथ वह बोला "लेकिन वो कहते हैं ना लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। ऐसे पागल लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे जो बस शिकायत करते रहते हैं …"
"तो क्या सरकार आप से कुछ नहीं कहती ?" आत्मविश्वास की कमी के बावजूद मैंने पूछा।
"सरकार?" उसकी आवाज थोड़ा गूंजी फिर उसने कुछ सोचते हुए अपने माथे पर उंगलियां फिराईं। फिर उसने अपना सिर हिलाया जैसे उसे कुछ याद आया हो: "अच्छा … तुम्हारा मतलब है वो लोग … वाशिंगटन वाले? ना वो मुझे तंग नहीं करते। वो अच्छे बन्दे हैं … उनमें से कुछ मेरे क्लब के सदस्य भी हैं। लेकिन उनसे बहुत ज्यादा मुलाकात नहीं होती … इसी वजह से ऐसा होना ही होता है कि कभी कभी मैं उनके बारे में भूल जाता हूं। ना वो मुझे तंग नहीं करते।" उसने अपनी बात दोहराई और मेरी तरफ उत्सुकता से देखते हुए पूछा:
"क्या आप कहना चाह रहे हैं कि ऐसी सरकारें भी होती हैं जो लोगों को पैसा बनाने से रोकती हैं?"
मुझे अपनी मासूमियत और उसकी बुद्धिमत्ता पर कोफ्त हुई।
"नहीं" मैंने धीमे से कहा "मेरा ये मतलब नहीं था ॰॰॰ देखिए सरकार ने कभी कभी तो सीधी सीधी डकैती पर लगाम लगानी चाहिए ना ॰॰॰"
"अब देखिए! " उसने आपत्ति की "ये तो आदर्शवाद हो गया। यहां यह सब नहीं चलता। व्यक्तिगत कार्यों में दखल देने का सरकार को कोई हक नहीं ॰॰॰"
(जारी है.)
(संवाद प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक 'पीले दैत्य का नगर' से)