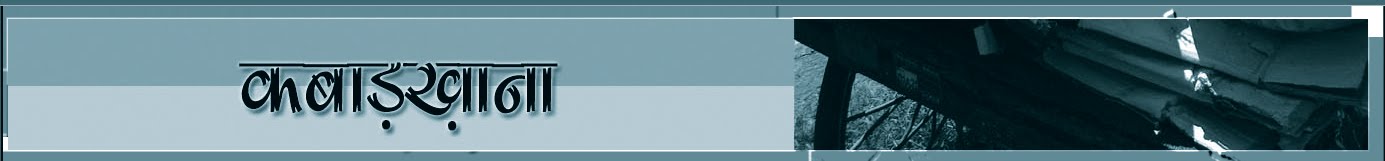Monday, December 31, 2007
हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों न ग़र्के़ दरिया
१९९४ में पाकिस्तान में रिलीज़ हुए अल्बम 'ग़ालिब का अन्दाज़-ए-बयां और' से सुनिये उन्हीं की गाई मिर्ज़ा असद की अतिविख्यात ग़ज़ल।
(*राग भूपाली में गाई हुई उस्ताद असद अमानत अली खान की बन्दिश 'लागे रे नैन तुम से पिया मोरे' को मैं कई वर्षों से तलाश रहा हूं। मेरे घर से कोई सज्जन उस पूरे संग्रह को ही पार कर ले गए थे। यदि कोई परोपकारी आत्मा मुझे उस बन्दिश तक पहुंच पाने की राह बता पाती तो मेरा साल बन जाता। )
Sunday, December 30, 2007
एक कबाडियों का किस्सा....

 फिर उसने कहा .....अल्लाह तुम पर मेहरबान हो! उसका करम तुम्हें नसीब हो!
फिर उसने कहा .....अल्लाह तुम पर मेहरबान हो! उसका करम तुम्हें नसीब हो!एक दिन, शेख अल-जुनैद यात्रा पर निकल पड़े। और चलते-चलते उन्हें प्यास ने आ घेरा। वे व्याकुल हो गये। तभी उन्हें एक कुआं दिखा, जो इतना गहरा था कि उससे पानी निकालना मुमकिन न था। वहां कोई रस्सी-बाल्टी भी न थी। सो उन्होंने अपनी पगड़ी खोली और साफे को कुएं में लटकाया। उसका एक छोर किसी कदर कुएं के पानी तक जा पहुंचा।
वे बार बार साफे को इसी तरह कुएं के भीतर लटकाते फिर उसे बाहर खींच कर अपने मुंह में निचोड़ते।
तभी एक देहाती वहां आया और उसने उनसे कहा-
`अरे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पानी से कहो कि ऊपर आ जाये। फिर तुम पानी अपने चुल्लू से पी लो।´
ऐसा कह कर वह देहाती कुएं के जगत तक गया और उसने पानी से कहा-
`अल्लाह के नाम पर तू ऊपर आ जा!´ और पानी ऊपर आ गया। और फिर शेख अल-जुनैद और उस देहाती ने पानी पिया।
प्यास बुझाने के बाद शेख अल-जुनैद ने उस देहाती को देखा और उससे पूछा-
`तुम कौन हो ?´
`अल्लाह ताला का बनाया एक बंदा।´ उसने जवाब दिया।
`और तुम्हारा शेख कौन है?´ अल-ज़ुनैद ने उससे पूछा।
`मेरा शेख है .....अल-जुनैद! हालांकि –आह! अभी तक मेरी आंखों ने उन्हें कभी देखा नहीं।´ गांव वाले ने जवाब दिया।
`फिर तुम्हारे पास ऐसी ताकत कैसे आयी?´ शेख ने उससे सवाल किया।
`अपने शेख पर मेरे यकीन की वजह से!´ उस सीधे-सादे देहाती ने जवाब दिया।
और चला गया!
छ्प्पन तोले की करधन के मालिक नए कबाड़ी का स्वागत

जंगली घोड़े की सवारी करो
हमारे समय के बड़े कवि-कथाकार श्री उदय प्रकाश ने कबाड़ख़ाने का सदस्य बनने का मेरा आग्रह स्वीकार किया है. उनका धन्यवाद.
अमरीका की मशहूर कवयित्री हाना कान (१९११-१९८८) की एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं :
जंगली घोड़े की सवारी करो
जंगली घोड़े की सवारी करो
जिस के पंख जामुनी
सियाह -सुनहरी धारियां
बस सिर ही
उसका सुर्ख लाल
जंगली घोड़े की सवारी करो
आकाश की तरफ़ जो उड़ रहा हो
ताकत से थामे रखो उस के पंख
इस के पहले कि तुम्हारी मौत हो जाए
या अधूरा रह जाए कोई काम
जंगली घोड़े की सवारी करो ज़रूर करो एक दफ़ा
और प्रविष्ट हो जाओ सूर्य के भीतर
हाना कान की बात आई है तो उन की कविता 'वंश वट' का अनुवाद यहां पढ़ाने का लोभ नहीं छोड़ पा रहा हूं:
मेरे दादाजी
जूते और वोदका
दाढ़ी और बाइबिल
भीषण सर्दियां
स्लेजगाड़ी और अस्तबल
मेरी दादी
नहीं था उस के पास
अपनी बेटी के लिए दहेज़
सो भेज दिया उसे
पानियों से भरे समुन्दर के पार
मेरी मां
दस घंटे काम करती थी
आधे डालर के लिए
हाड़ तोड़ देने वाली उस दुकान में
मेरी मां को मिला एक विद्वान
मेरे पिता
वे जीवित रहे किताबों,
शब्दों और कला पर;
लेकिन ज़रा भी दिल नहीं था
मकानमालिक के पास
मैं
मैं कुछ हिस्सा उन से बनी हूं
कुछ हिस्से में दूने हैं वो
हालांकि तंग बहुत किया
अपनी मां को मैंने
Friday, December 28, 2007
आज जो पढ़ा,आज जो सोचा
" यह बिल्कुल सच है कि मैं फिर कभी कविता और चित्रों के फेर से निकल नहीं पाया. और कहनियां भी. ये सब मेरे अकेलेपन और असुरक्षा के एकमात्र शरण्य बन जायेंगे ऐसा मैंने उन दिनों बिल्कुल नहीं सोचा था. बाद में मैनें कहीं पढा,शायद इतालवी कव इयूजीन मोंताले ने कहा था कि कवि असुरक्षा का जादूगर होता है.वह अपने जय को पराजय और पराजय में बदलने के एक अंतहीन काम में जीवन भर लगा रहता है. वह बहुत अशक्त होता है लेकिन अपने दुखों और निर्वासन की गुफा में कैद उसकी आंखें किसी अपराजेय सम्राट् की तरह आकाश की ओर हमेशा लगी रहती हैं. मेरी अपनी कविता की पंक्ति है कि रात के अकेलेपन में कवि का शरीर चंद्रमा की तरह चमकता है.
कविता ही नहीं किसी भी कला की सृजनात्मकता के गहन पलों में समूचा युग और संसार कवि के स्नायु में किसी द्रव की तरह बहता है.
और जिसका शरीर रात में चंद्रमा की तरह नहीं चमकता ,जो एक अपराजेय सम्राट् की तरहा काश को नहीं ताकता ,काल और संसार जिसकी शिराओं में द्रव की तरह नहीं प्रवाहित ,उसे मैं कभी भी कवि नही मान पाता.चाहे वह कितना भी बड़ा संपादक ,पत्रकार ,राज्नीतिक नेता या अफसर क्यों न हो.
कविता की सत्ता तमाम बाहरी सत्ताओं का विरोध करती है. वह बहुत गहरे अर्थ और प्राचीन अर्थों में नैतिक होती है."
(भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार प्राप्त कविताओं के संग्रह 'उर्वर प्रदेश' में उदय प्रकाश के वक्तव्य का एक अंश)
इच्छा
मुझे हवा चाहिये
जिसमें आजाद होकर मैं सांस ले सकूं
और जिसे गुंजा सकूं
अपने शब्दों से
मुझे घर चहिये
जिसके लोग मुझे प्यार करें
और जहां मैं नाराज हो सकूं
मनाये जाने के लिये
मुझे नीला आसमान चहिये
जिसके नीचे
मैं हरियाली की तरह फैल सकूं
और चूम सकूं उस लड़की को
अपने होठों की पूरी ऊष्मा के साथ -
मुझे खुले हाथ और सधी हुई उंगलियां चाहिये
जिनसे मैं उकेर सकूं
इतिहास की सुन्दरतम कलाकृति
और बजा सकूं
संगीत का सबसे जटिल राग
इन सबके अलावा
मुझे चाहिये एक नश्वर देह
जिसे मैं अपने पापों से गन्दा कर सकूं
और जिसके खत्म होने तक
मैं आदमी की तरह जी सकूं
(यह कविता मेरे अजीज दोस्त अशोक पान्डे के संग्रह 'देखता हूं सपने' से ली गई है,बिना किसी आभार के. साथ ही इस हिदायत के साथ कि भइए उठ अपनी खटारा साइकिल उठा,तराजू -बाट दुरुस्त कर और फेरा लगा.बाबू जी! कबाड़खाने में कोई सोना-चांदी तो ना गेरेगा.आएगा तो लोया ,पिलाट्टिक और रद्दी पेप्पोर ही.हम तो इसी में से काम का 'माल'छांट कर अपनी दुकान चलायेंगे. देख तो आजू-बाजू क्या हो रिया है और तू खुन्नस खा के सो रिया है. चल काम पे लग नहीं तो पिटैगा और 'पीसे' भी ना मिलैंगे....टेंशन काय को लेने का....नराई,प्यार और पुच्च....)
11 साल के बच्चे की पहली हिंदी पोस्ट
तारेजमीं पर फिल्म देखी। वो भी चाणक्या में। सिनेमा हॉल हमेशा के लिए बंद होने से एक दिन पहले। फिल्म अच्छी थी। लेकिन और अच्छी हो सकती थी। इसका अंत दूसरी तरह से होना चाहिए था।
लेकिन फिल्म तो अच्छी तब बनती जब ईशान अच्छा पेंटर भी नहीं बनता या कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता तो भी लोग उसे समझते और प्यार देते। हर बच्चा कुछ न कुछ बहुत अच्छा करे ये उम्मीद नहीं करना चाहिए। ये जरूरी तो नहीं है कि वो कुछ बढ़िया करे ही। कोई भी बच्चा एवरेज हो सकता है, एवरेज से नीचे भी हो सकता है। लेकिन इस वजह से कोई उसे प्यार न दे ये तो गलत है।
पिंजरे में मुनिया
उस दौर की राजनीति का एक दृष्य लिखा था । देखें , कि आज के दौर
से मिलती-जुलती सी लगती है या नहीं वो सूरत ।
मुंशी कि क्लर्क या ज़मींदार
लाज़िम है कलेक्टरी का दीदार
हंगामा ये वोट का फ़क़त है
मतलूब हरेक से दस्तख़त है
हर सिम्त मची हुई है हलचल
हर दर पे शोर है कि चल-चल
टमटम हों कि गाड़ियां कि मोटर
जिस पर देको, लदे हैं वोटर
शाही वो है या पयंबरी है
आखिर क्या शै ये मेंबरी है
नेटिव है नमूद ही का मुहताज
कौंसिल तो उनकी हि जिनका है राज
कहते जाते हैं, या इलाही
सोशल हालत की है तबाही
हम लोग जो इसमें फंस रहे हैं
अगियार भी दिल में हंस रहे हैं
दरअसल न दीन है न दुनिया
पिंजरे में फुदक रही है मुनिया
स्कीम का झूलना वो झूलें
लेकिन ये क्यों अपनी राह भूलें
क़ौम के दिल में खोट है पैदा
अच्छे अच्छे हैं वोट के शैदा
क्यो नहीं पड़ता अक्ल का साया
इसको समझें फ़र्जे-किफ़ाया
भाई-भाई में हाथापाई
सेल्फ़ गवर्नमेंट आगे आई
पंव का होश अब फ़िक्र न सर की
वोट की धुन में बन गए फिरकी
-अकबर इलाहाबादी
(1.दर्शन.2.वांछित.3.तरफ.4.पैगंबरी.5.वस्तु.6.सामने आना.7.गैर लोग.8.दीवाने.9.किफ़ायत का फ़र्ज़)
(हक तो नहीं बनता अशोक भाई ,राजेशजी वाले स्नेह संबोधन को बोलने का मगर आपकी इस उचाटभरी नाराजगी के बाद मनाने के लिए मुझे भी कहना पड़ रहा है - अब मान जा रे , पंडा।टिप्पणी जा नहीं रही है इसलिए पोस्टिंग आप्शन ही काम में ले रहा हूं। )
अजित वडनेरकर
यूँ लाद चलोगे पंडा जी ?

इस क़िस्से को लगभग डेढ़ दशक हो चुका है. हो सकता है इससे कुछ अधिक ही समय हुआ हो. लेकिन इस मरणासन्न ब्लॉग के पाठकों के हितार्थ यहाँ एक बार फिर याद किया जा रहा है.
नैनीताल शहर में तल्लीताल के एक पाताललोक जैसी खोह से पतले-झिल्ले कागजों में, हैंडसैटिंग प्रेस की मदद से छपने वाला हमारा पाक्षिक अखबार 'नैनीताल समाचार' एक समय मरणासन्न हो चला था. अखबार चलाने लायक पैसे थे नहीं, व्यापारी लोग विज्ञापन क्यों देते, अखबार पढ़ने वाले अपनी या बच्चों की फीस ही मुश्किल से दे पाते थे, अखबार को डोनेशन क्या देते. अंततः संपादक-मालिक-कार्यकर्ता-संवाददाता और आंदोलनकारी राजीव लोचन साह ने पाठकों के नाम एक अपील छाप ही दी. अब उसकी ठीक ठीक इबारत याद नहीं लेकिन भाव कुछ यूँ था कि बस भई, अब नहीं चल सकता. नैनीताल समाचार बंद करना पड़ रहा है क्योंकि उसके छापने लायक खर्च हमारे पास नहीं है.
आज 2007 में भी नैनीताल समाचार जिंदा है, चल रहा है, लगातार निकल रहा है. तो फिर संपादक की उस मार्मिक अपील के बाद ऐसा क्या हुआ कि अखबार बंद नहीं हुआ? राजीव लोचन साह तल्लीताल में ही मिल जाएँगे. कभी वहाँ जाना हो तो उनसे पूछिएगा. वो बताएंगे कि अखबार बंद करने की उस सूचना के बाद थैले के थैले भर भर कर चिट्ठियाँ उनके पास पहुँचने लगीं कि -- वाह, वाह, आप कौन होते हैं समाचार बंद करने वाले. समाचार हमारा है, और चलेगा.
जनाब-ए-आली, किस्सा मुख्तसर ये कि समाचार आज भी चल रहा है और पूरे जोशो खरोश के साथ.
अशोक पांडे, जिसे मैं हमेशा प्यार से पंडा कहता आया हूँ, अब कह रहा है कि कबाड़खाना नहीं चलेगा. मेरा जवाब सुन लिया जाएः वाह, वाह, तुम कौन होते हो पंडा जी, अपनी मर्जी से कबाड़खाना बंद करने वाले और ये कहने वाले कि मेरा रामनगर और बाकी आपकी सभी पोस्टें 31 दिसंबर से हटा ली जाएँगी. और ये भी कहने वाले कि अब मैं चला, आप लोग चलाइए ब्लाग.
ये समझ लो मियां कि शुरू करना तो तुम्हारे हाथ में था, अब उसे बंद करना कतई तुम्हारे बस में नहीं है. ये गाड़ी तो अब छूट चुकी है तल्लीताल डाँठ से. अब कहते हो कि मैं इसमें नहीं बैठूंगा. भई, तुम्हें उतरने कौन दे रहा है.
एकतरफा ऐलान करके यूँ लाद चलोगे पंडा जी? और सोच रहे हो कि कोई कुछ बोलेगा नहीं?
और जो ये बेनामी सज्जन तो इधर उधर बीट कर रहे हैं, ये तो हमारी रामलीला के एक्स्ट्रा आर्टिस्ट हैं भई. इनके कारण कबाड़खाना बंद हो नहीं सकता बल्कि इन्हीं के कारण चलता रहेगा. कुछ कड़वी बहसों की शुरुआत इन्हीं के बहाने सही.
अब मान जा रे, पंडा.
Thursday, December 27, 2007
बना रहे कबाड़खाना
निवेदन है कि आप पुनर्विचार करें। विवाद तो कई हैं, होते रहते हैं, होने भी चाहिए। ट्रांजिशन के दौर से गुजरता देश, समाज, संस्कृति, भाषा, परिवार ये सब कुछ तो विवादों में है। हिंदी में नुक्ते के इस्तेमाल को लेकर कितनी कड़वी बहसें हो चुकी है। हिंदी में अरबी फारसी और तुर्की के शब्द भी विवादों में रहे हैं। यूरोपीय भाषा के शब्दों को लेकर भी अलग अलग विचार हैं। भाषा में लोक और अभिजन की बहस है। भाषा में गाली क्यों न हो, के मजबूत तर्क हैं और क्यों हो के भी उतने ही जोरदार तर्क हैं।
और फिर अंतिम सत्य तो अमूर्त है न अशोक भाई, तो अपने अपने सच को लेकर क्यों न बने रहे दुनिया के इस खेल में। कबाड़खाना बना रहे, इसमें मेरा स्वार्थ है। कुछ चीजें जो यहां मिलती हैं, वो अन्यत्र नहीं मिलती। -दिलीप मंडल
कबाड़ी की आखि़री पोस्ट
यह न कोई मिशन था न कोई उदात्त कर्म. बस एक नए माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाने का मोह (या लालच) था.
२४ तारीख को मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन था. मैंने एक पोस्ट लगाई थी उस आनन्द के प्रति रफ़ी साहब का आभार व्यक्त करते हुए जो उनकी आवाज़ ने कम से कम मुझे तो इतने सालों से लगातार दिया है.
एक कोई बेनाम सज्जन को एक ऐसे शब्द से आपत्ति है जिसका इस्तेमाल पोस्ट की टाइटिल में हुआ है.
माफ़ करेंगे. थोड़ा संवेदनशील हूं. डरपोक नहीं हूं.
बहुत भूमिकाएं नहीं बांधूंगा.
मैं ३१ दिसम्बर से कबाड़ख़ाने से अपना नाम वापस ले रहा हूं. मेरे अलावा इस ब्लाग पर इन तमाम सज्जनों ने अपना नाम बतौर कबाड़ी देने की इजाज़त दी थी: राजेश जोशी (बीबीसी लन्दन में कार्यरत), शिरीष मौर्य (कवि, अनुवादक, अध्यापक), शैलेन्द्र जोशी (कवि, अनुवादक), अविनाश (मीडिया से सम्बद्ध, मोहल्ला नामक ब्लाग चलाते हैं), अजित वडनेरकर (मीडिया से सम्बद्ध, शब्दों का सफ़र नामक ब्लाग चलाते हैं), दिनेश पालीवाल (कम्प्यूटर एक्सपर्ट), दीपा पाठक (मीडिया से सम्बद्ध, हिसालू काफ़ल नामक ब्लाग चलाती हैं), आशुतोष ('हिन्दुस्तान' में कार्यरत, बुग्याल नामक ब्लाग चलाते हैं, मेरे पहले गुरुओं में), सुन्दर ठाकुर (कवि, 'नवभारत टाइम्स' से संबद्ध), इरफ़ान (रेडियो और संगीत और कविता और तमाम इलाकों के जानकार, अभिन्न मित्र, मुख्यत: 'टूटी हुई, बिखरी हुई' और 'सस्ता शेर' नामक ब्लाग चलाते हैं), वीरेन डंगवाल (साहित्य अकादेमी पुरुस्कार से सम्मानित हिन्दी और देश के सबसे बेहतरीन कवियों में एक, महान मित्र और मेरे अपने बरगद), चन्द्रभूषण (मीडिया से सम्बद्ध, पहलू नामक ब्लाग चलाते हैं), विनीता यशस्वी (नैनीताल में मीडिया से सम्बद्ध), भूपेन (मीडिया से सम्बद्ध, काफ़ीहाउस नामक ब्लाग चलाते हैं), काकेश (काकेश की कतरनें नामक ब्लाग चलाते हैं), आशीष (मुक्तेश्वर के पास एक रेसोर्ट चलाते हैं), सिद्धेश्वर (हिन्दी पढ़ाते हैं, मेरे पहले गुरुओं में), रोहित उमराव (फ़ोटोपत्रकार), दिलीप मंडल (मीडिया से सम्बद्ध, ब्लागिंग में जाना माना प्रतिबद्ध नाम), कथाकार (सूरज प्रकाश, कथाकार नामक ब्लाग चलाते हैं, आजकल एक भीषण दुर्घटना का शिकार होने के बाद स्वास्थ्यलाभ कर रहे हैं) और अरुण रौतेला (नैनीताल में वकालत करते हैं).
यह पोस्ट इन सभी सज्जनों को सविनय सूचना है कि मैं आप सब को कबाड़ख़ाने का एडमिनिस्ट्रेटर बना रहा हूं. मेरी यह अंतिम पोस्ट है. ३१ दिसम्बर से मैं अपना नाम कबाड़ख़ाने से हटा लूंगा.
यदि इन सज्जनों को कबाड़खाना चलाने में कोई दिलचस्पी न हो तो उसी दिन से यह ब्लाग हटा लेने पर सभी को सहमत समझ लिया जाएगा.
सभी पाठकों का धन्यवाद.
*'सुख़नसाज़' ३१ दिसम्बर से हटा लिया जाएगा. और 'मेरा रामनगर भी.
Wednesday, December 26, 2007
'कौन इस शहर में दीवाना हुआ मेरे बाद' उर्फ राही और नीरज के शहरनामे पर क्षण भर
बन गया तकलीद से मेरी ये सौदाई अबस
( ग़ालिब)
शहरनामा लिखने की वैसी सुदीर्घ और प्रौढ़ परम्परा के दर्शन हिन्दी में नहीं होते हैं जैसी कि वह उर्दू साहित्य में दिखाई देती हैऐसा नहीं है कि हिन्दी साहित्य में 'नगर शोभा वर्णन' के रंग-प्रसंग नहीं हैं और न ही यह कि नगरों-शहरों की स्मृति-विस्मृति में हिन्दी वालों ने कोई कम आंसू बहाए हैं फिर भी पहली नजर में ऐसा लगता है कि शहर दर शहर भटकने, उजड़ने, बसने, बिखरने और बनने की जो जद्दोजहद आरम्भ से ही उर्दू भाषा और साहित्य से जुड़े तमाम घटकों के अनुभव जगत का यथार्थ बनी लगभग वैसा ही 'कितने शहरों में कितनी बार' का वाकया या हादसा हिन्दी के हिस्से में शायद नहीं आयाअपनी पुस्तक 'उर्दू भाषा और साहित्य'में काव्य-शास्त्र संबंधी कुछ बातों का उल्लेख करते हुए फिराक गोरखपुरी लिखते हैं-'शहर आशोब (में)किसी शहर के उजड़ने या बरबाद हो जाने पर उसके पुराने वैभव को दुःख के साथ याद किया जाता हैइस प्रकार की कविता अत्यन्त मार्मिक होती है'उर्दू काव्य में शहरे-चराग़ां,शहरे-ख़ामोशां,शहरे-आरजू वगैरह का न केवल जिक्र आया है या कि किसी शहर के तसव्वुर में फकत 'वाह्-वाह् या 'हाय-हाय' ही की गई है बल्कि उसके समुचित वैविध्य,विस्तार और वर्णन के साथ यादगार कलात्मक प्रस्तुति भी की गई है
नास्टैल्जिया शहरनामे का केन्द्रीय सूत्र है जिसके रेशे-रेशे को उधेड्ना ही उसे दोबारा बुनना हैग़ालिब के शब्दों में कहें तो यह 'जले हुए जिस्म और दिल की जगह की राख को कुरेदने की जुस्तजू'हैशहरनामा न तो संस्मरण है और न ही यात्रा वृतांत अपितु मुझे लगता है कि यह किसी शहर से जुड़ी स्मृतियों के कबाड़खाने को खंगालते हुए एक-एक चीज को उलट-पुलट कर जस का तस रख देने का कलात्मक कारनामा है
'चांद तो अब भी निकलता होगा' राही मासूम रज़ा की एक तवील नज़्म है जो राही का 'शहरनामा अलीगढ़'भी कहा जा सकता हैवही अलीगढ़,वही राही का 'शहरे-तमन्ना' जिसकी यूनिवर्सिटी को उन्होंने दूसरी मां का दर्जा दिया थागंगौली,गाजीपुर और अलीगढ़ राही के व्यक्तित्व-निर्माण की भूमियां हैंअलीगढ़ में उन्होंने 'छोटे आदमी की बड़ी कहानी'शीर्षक से परमवीर अब्दुल हमीद की जीवनी लिखी,'आधा गांव' जैसा कालजयी उपन्यास लिखा और अपने पूरे दोस्त कुंवर पाल सिंह को समर्पित कियाइसी अलीगढ़ को उन्होंने अपने उपन्यास 'टोपी शुक्ला' में अमर कर दिया और यह वही अलीगढ़ है जिसके 'कूए यार' से रुस्वा होकर उन्हें बंबई या मुंबई के 'सूए दार, की जानिब चलना पड़ा जहां फिल्मी दुनिया के चकाचौंध में अपनी कलम के बूते एक अपरिहार्य जगह बनाकर रहते हुए भी वे निरंतर अपने शहरे-तमन्ना को याद करते रहे -
कुछ उस शहरे-तमन्ना की कहो
ओस की बूंद से क्या करती है अब सुबह सुलूक
वह मेरे साथ के सब तश्ना दहां कैसे हैं
उड़ती-पड़ती ये सुनी थी कि परेशान हैं लोग
अपने ख्वाबों से परेशान हैं लोग
****
जिस गली ने मुझे सिखलाए थे आदाबे-जुनूं
उस गली में मेरे पैरों के निशां कैसे हैं
शहरे रुसवाई में चलती हैं हवायें कैसी
इन दिनों मश्गलए-जुल्फे परीशां क्या है
साख कैसी है जुनूं वालों की
कीमते चाके गरीबां क्या है
****
कौन आया है मियां खां की जगह
चाय में कौन मिलाता है मुहब्बत का नमक
सुबह के बाल में कंघी करने
कौन आता है वहां
सुबह होती है कहां
शाम कहां ढ़लती है
शोबए-उर्दू में अब किसकी ग़ज़ल चलती है
****
चांद तो अब भी निकलता होगा
मार्च की चांदनी अब लेती है किन लोगों के नाम
किनके सर लगता है अब इश्क का संगीन इल्जाम
सुबह है किनके बगल की जीनत
किनके पहलू में है शाम
किन पे जीना है हराम
जो भी हों वह
तो हैं म्रेरे ही कबीले वाले
उस तरफ हो जो गुजर
उनसे ये कहना
कि मैंने उन्हें भेजा है सलाम
राही मासूम रज़ा के महाकाव्य '१८५७'(बाद में 'क्रांति कथा' नाम से प्रकाशित) की भूमिका'गीतों का राजकुमार'कहे जाने वाले नीरज ने लिखी थी कवि सम्मेलनों ,किताबों,कैसेटों के माध्यम से हिन्दी कविता को आम आदमी की जुबान तक पहुंचाने वाले कवि नीरज ने अपार लोकप्रियता हासिल की हैवे कविता की लोकप्रियता के जीवित कीर्तिमान है लेकिन उनकी यही लोकप्रियता हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों की दृष्टि में 'शाप' बन गई('लोकप्रियता बनाम साहित्यिकता' के मुद्दे को हिन्दी के साहित्यिक विमर्श का विषय कभी बनने ही नहीं दिया गया और यदि कभी ऐसा हुआ भी तो उस पर कोई गंभीर चर्चा शायद ही कभी हुई होहां,'पापुलर कल्चर' के अध्येता अब इस पर बात जरूर कर रहे हैं)राही अलीगढ़ छोड़कर मुंबई गये और नीरज कानपुर छोड़कर अलीगढ़ आएराही फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाकर वहीं के हो गये और नीरज फिल्मी दुनिया का फेरा कर "कांरवां गुजर गया गुबार देखते'हुए अलीगढ़ लौट आए,पर कानपुर को भूल नहीं पाएअपने शहरे तमन्ना को कोई भूलता है भला! प्रस्तुत है नीरज के शहरनामा 'कानपुर के प्रति' के कुछ अंश -
कानपुर!आह!आज तेरी याद आई फिर
स्याह कुछ और मेरी रात हुई जाती है
आंख पहले भी यह रोई थी बहुत तेरे लिये
अब तो लगता है कि बरसात हुई जाती है
****
और ऋषियों के नाम वाला वह नामी कालिज
प्यार देकर भी न्याय जो न दे सका मुझको
मेरी बगिया की हवा जो तू उधर से गुजरे
कुछ भी कहना न,बस सीने से लगाना उसको
****
बात यह किन्तु सिर्फ जानती है 'मेस्टन रोड'
ट्यूब कितने कि मेरी साइकिल ने बदले हैं
और 'चित्रा' से जो चाहो तो पूछ लेना यह
मेरी तस्वीर में किस किसके रंग धुंधले हैं
****
शोख मुस्कान वही और वही ढीठ नजर
साथ सांसों के यहां तक रे! चली आई है
तीन सौ मील की दूरी भी कोई दूरी है
प्रेम की गांठ तो मरके भी न खुल पई है
****
कानपुर ! आज जो देखे तू अपने बेटे को
अपने 'नीरज' की जगह लाश उसकी पायेगा
सस्ता कुछ इतना यहां मैंने खुद को बेचा है
मुझको मुफलिस भी खरीदे तो सहम जायेगा
(हर्ष,विषाद,उल्लास, उपालंभ,मान-अभिमान की काव्यात्मक कारगुजारियों से गुजरते हुए मैं यहां राही मासूम रज़ा और नीरज के शहरनामे के बहाने अपने उस शहरनामे को भी भीतर ही भीतर दोहरा लेना चाहता हूं जो पिछले कई सालों से लगातार लिखा जा रहा है; बकौल अपने प्रिय शायर इब्ने इंशा-
किसका-किसका हाल सुनाया तू ने ऐ अफसानागो
हमने एक तुझी को ढुंढा इस सारे अफसाने में)
Monday, December 24, 2007
हैप्पी बर्थडे रफ़ी साहब

 मेरे बचपन और लड़कपन और जवानी और पहली मोहब्बत और पहले विरह और पहले प्रवास और जाने कितने कितने मरहलों पर मुझे अहसास हुआ है कि मोहम्मद रफ़ी साहब को याददाश्त से हटा दूं तो मेरे जीवन का बड़ा हिस्सा भूसे का ढेर बन जाएगा.
मेरे बचपन और लड़कपन और जवानी और पहली मोहब्बत और पहले विरह और पहले प्रवास और जाने कितने कितने मरहलों पर मुझे अहसास हुआ है कि मोहम्मद रफ़ी साहब को याददाश्त से हटा दूं तो मेरे जीवन का बड़ा हिस्सा भूसे का ढेर बन जाएगा.आज मोहम्मद रफ़ी साहब की ८३वीं सालगिरह है.
*रफ़ी साहब को इन जगहों पर भी सुनें:
http://kabaadkhaana.blogspot.com/2007/12/blog-post_13.html
http://kabaadkhaana.blogspot.com/2007/12/blog-post_1848.html
http://sukhansaaz.blogspot.com/2007/12/blog-post_4012.html
http://sukhansaaz.blogspot.com/2007/12/blog-post_09.html
Sunday, December 23, 2007
बधाई नरेन्द्र भाई
देखो कितनी सक्षम है यह अब भी बनाए हुए अपने आप को चाक-चौबन्द -
हमारी शताब्दी की नफ़रत।
किस आसानी से कूद जाती है यह
सबसे ऊंची बाधाओं के परे।
किस तेज़ी से दबोच कर गिरा देती है हमें।
बाकी भावनाओं जैसी नहीं होती यह।
यह युवा भी है और बुज़ुर्ग भी।
यह उन कारणों को जन्म देती है
जो जीवन देते हैं इसे।
जब यह सोती है, स्थाई कभी नहीं होती इसकी नींद
और अनिद्रा इसे अशक्त नहीं बनाती;
अनिद्रा तो इस का भोजन है।
एक या कोई दूसरा धर्म
इसे तैयार करता है - तैनात।
एक पितृभूमि या दूसरी कोई
इसकी मदद कर सकती है - दौड़ने में!
शुरू में न्याय भी करता है अपना काम
जब तक नफ़रत रफ़्तार नहीं पकड़ लेती।
नफ़रत, नफ़रत
एन्द्रिक आनन्द में खिंचा हुआ इसका चेहरा
और बाकी भावनाएं -कितनी कमज़ोर, किस कदर अक्षम।
क्या भाईचारे के लिए जुटी कभी कोई भीड़?
क्या सहानुभूति जीती कभी किसी दौड़ में?
क्या सन्देह से उपज सकता है भीड़ में असन्तोष?
केवल नफ़रत के पास हैं सारे वांछित गुण -
प्रतिभा, कड़ी मेहनत और धैर्य।
क्या ज़िक्र किया जाए इस के रचे गीतों का?
हमारे इतिहास की किताबों में कितने पन्ने जोड़े हैं इस ने?
तमाम शहरों और फ़ुटबाल मैदानों पर
आदमियों से बने कितने गलीचे बिछाए हैं इस ने?
चलें: सामना किया जाए इस का:
यह जानती है सौन्दर्य को कैसे रचा जाए।
आधी रात के आसमान पर आग की शानदार लपट।
गुलाबी सुबहों को बमों के अद्भुत विस्फ़ोट।
आप नकार नहीं सकते खंडहरों को देखकर
उपजने वाली संवेदना को -
न उस अटपटे हास्य को
जो उनके बीच महफ़ूज़ बचे
किसी मजबूत खंभे को देख कर महसूस होता है।
नफ़रत उस्ताद है विरोधाभासों की -
विस्फ़ोट और मरी हुई चुप्पी
लाल खून और सफ़ेद बर्फ़।
और सब से बड़ी बात - यह थकती नहीं
अपने नित्यकर्म से - धूल से सने शिकार के ऊपर
मंडराती किसी ख़लीफ़ा जल्लाद की तरह
हमेशा तैयार रहती है नई चुनौतियों के लिए।
अगर इसे कुछ देर इंतज़ार करना पड़े तो गुरेज़ नहीं करती
लोग कहते हैं नफ़रत अंधी होती है।
अंधी?
छिपे हुए निशानेबाज़ों जैसी
तेज़ इसकी निगाह - और बगैर पलक झपकाए
यह ताकती रहती है भविष्य को
-क्योंकि ऐसा बस यही कर सकती है।
* नोबेल पुरुस्कार विजेता पोलिश कवयित्री विस्वावा शिम्बोर्स्का की एक और कविता।
मसखरों को अन्तरिक्ष में मत ले जाओ
मसखरों को अन्तरिक्ष में मत ले जाओ
यह मेरी सलाह है
चौदह बेजान नक्षत्र
कुछेक पुच्छल तारे, दो सितारे
जब तक तुम तीसरे सितारे की तरफ चलने लगोगे
तुम्हारे मसखरों के लतीफों का खज़ाना चुक चुका होगा
आकाशगंगा वही है जो वह है -
यानी सम्पूर्ण।
तुम्हारे मसखरे इसे कभी माफ़ नहीं करेंगे।
उन्हें किसी चीज़ से खुशी नहीं मिलेगी:
न समय से (जो इस कदर सीमाहीन है)
न सौन्दर्य से (जिस में कोई खोट नहीं)
न गुरुत्व से (जिस में कोई हल्कापन नहीं)
जब दूसरों के चेहरों पर असीम अचरज नज़र आएगा
मसखरे उबासियां ले रहे होंगे।
चौथे सितारे के रास्ते में
चीज़ें और भी बदतर हो जाएंगी
जम चुकी मुस्कानें
बाधित नींद और असन्तुलन
फ़िज़ूल की बकबक:
याद करो उस कौए को जिसकी चोंच में पनीर क टुकड़ा था
महाराजाधिराज के चित्र पर मक्खियों की टट्टी
स्टीमबाथ में बंदर-
असल में जीवन तो वह था।
संकीर्ण विचारों वाले वे मसखरे
अनंतता पर तरजीह देंगे गुरुवार को, किसी भी दिन।
वे - आदिकालीन।
अन्तरिक्ष के गोलों के संगीत से उन्हें बेहतर लगेगा बेसुरापन।
वे प्रसन्नतम रहते हैं
सिद्धान्त और वास्तविकता की दरारों के बीच
कारण और प्रभाव की दीवारों के बीच।
लेकिन यह शून्य है, धरती नहीं:
यहां हर चीज़ सम्पूर्ण है।
तेरहवें नक्षत्र पर
(उसके दोषहीन एकान्त पर निगाह डालते हुए)
वे अपने दड़बों से बाहर निकलने से इन्कार कर देंगे :
"मुझे सरदर्द है" वे शिकायत करेंगे
"मेरे पैर का अंगूठा दब गया"
क्या बर्बादी है। कितनी शर्म की बात
बाहरी अन्तरिक्ष में तबाह किया जा रहा इतना सारा धन।
*यह कविता नोबेल पुरुस्कार से सम्मानित पोलिश कवयित्री विस्वावा शिम्बोर्स्का की है। आज इस के और इस के बात लगाई जाने वाली कविता के लिए कोई सन्दर्भ और प्रसंग बताने की ऐसी कोई दरकार है, मुझे नहीं लगता।
'तान कप्तान की ऐसी फिरत है जैसे अर्जुन जी के बान'
नुसरत साहब के वालिद यानी फ़तेह अली ख़ान साहेब न सिर्फ़ बड़े क़व्वाल थे, उन्हें ध्रुपद में कमाल हासिल था. उनकी तानें जगतख्यात थीं और कालान्तर में वे 'तान कप्तान' के नाम से जाने गए. (*असल में यह भी सच नहीं है. 'तान कप्तान' की पदवी पटियाला घराने के फ़तेह अली ख़ान साह्ब के दादाजी को कहा जाता था. यह सूचना अभी अभी टैक्सास में अध्ययनरत श्री नीरज ने दी है. 'अन्तर्ध्वनि नामका ब्लाग चलाने वाले नीरज भाई ने एक लिन्क भी भेजा है : http://www.sawf.org/Newedit/edit12112000/musicarts.asp . यह ब्लागिंग का एक और ज़बर्दस्त आयाम है. फ़िल्हाल नीरज भाई का शुक्रिया.)
प्रस्तुत है राजन साजन मिश्र की थर्रा देने वाली आवाज़ों में राग अडाना में यह शानदार कम्पोज़ीशन जिसके बोल उस्ताद फ़तेह अली ख़ान के दादाजी का महिमागान करते हैं: "तान कपतान, छा गयो जग में फ़तेह अली ख़ान"
(१० मिनट ११ सेकेंड)
*यह पोस्ट विमल भाई के लिये खास ('सोनार तेरी सोना पर मेरी बिस्वास है' पर बिस्वास करते हुए और उनका आभार भी व्यक्त करते हुए.)
हमारी संस्कृति और जाति व्यवस्था को मत छेड़ो प्लीज़...
क्या देश के बीते लगभग एक हजार साल के इतिहास की हम ऐसी कोई सरलीकृत व्याख्या कर सकते हैं? ऐसे नतीजे निकालने के लिए पर्याप्त तथ्य नहीं हैं। लेकिन हाल के वर्षों में कई दलित चिंतक ऐसे नतीजे निकाल रहे हैं और दलित ही नहीं मुख्यधारा के विमर्श में भी उनकी बात सुनी जा रही है। इसलिए कृपया आंख मूंदकर ये न कहें कि ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है।
भारत में इन हजार वर्षों में एक के बाद एक हमलावर आते गए। लेकिन ये पूरा कालखंड विदेशी हमलावरों का प्रतिरोध करने के लिए नहीं जाना जाता है। प्रतिरोध बिल्कुल नहीं हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता लेकिन समग्रता में देखें तो ये आत्मसमर्पण के एक हजार साल थे। क्या हमारी पिछली पीढ़ियों को आजादी प्रिय नहीं थी? या फिर अगर कोई उन्हें अपने ग्रामसमाज में यथास्थिति में जीने देता था, उनकी पूजा पद्धति, उनकी समाज संरचना, वर्णव्यवस्था आदि को नहीं छेड़ता था, तो वो इस बात से समझौता करने को तैयार हो जाते थे कि कोई भी राजा हो जाए, हमें क्या?
ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर इसका जवाब ढूंढने की कोई कोशिश अगर हुई है, तो वो मेरी जानकारी में नहीं है। देश की लगभग एक हजार साल की गुलामी की समीक्षा की बात शायद हमें शर्मिंदा करती है। हम इस बात का जवाब नहीं देना चाहते कि हजारों की फौज से लाखों की फौजें कैसे हार गई। हम इस बात का उत्तर नहीं देना चाहते कि कहीं इस हार की वजह ये तो नहीं कि पूरा समाज कई स्तरों में बंटा था और विदेशी हमलावरों के खिलाफ मिलकर लड़ने की कल्पना कर पाना भी उन स्थितियों में मुश्किल था? और फिर लड़ने का काम तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सिर्फ एक वर्ण का काम है!
इतिहास में झांकने का मकसद अपनी पीठ पर कोड़े मारकर खुद को लहूलुहान कर लेना कतई नहीं हो सकता, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गलतियों से न सीखने वाले दोबारा और अक्सर ज्यादा बड़ी गलतियां करने को अभिशप्त होते हैं।
भारत पर राज करने शासकों में से शुरूआती मुगल शासकों ने अपेक्षाकृत निर्बाध तरीके से (हुमायूं के शासनकाल के कुछ वर्षों को छोड़कर) देश पर राज किया। मुगल शासकों ने बाबर के समय से ही तय कर लिया था कि इस देश के लोग अपना जीवन जिस तरह चला रहे हैं, उसमें न्यूनतम हस्तक्षेप किया जाए। जजिया टैक्स लगाना उस काल के हिंदू जीवन में एकमात्र ऐसा मुस्लिम और शासकीय हस्तक्षेप था, जिससे आम लोगों को कुछ फर्क पड़ता था। ये पूरा काल अपेक्षाकृत शांति से बीता है। औरंगजेब ने जब हिंदू यथास्थिति को छेड़ा तो मुगल शासन के कमजोर होने का सिलसिला शुरू हो गया।
उसके बाद आए अंग्रेज शासकों ने भारतीय जाति व्यवस्था का सघन अध्ययन किया। उस समय के गजेटियर इन अध्ययनों से भरे पड़े हैं। जाति व्यवस्था की जितनी विस्तृत लिस्ट आपको अंग्रेजों के लेखन में मिलेगी, उसकी बराबरी समकालीन हिंदू और हिंदुस्तानी लेखन में भी शायद ही कहीं है। एक लिस्ट देखिए जो संयुक्त प्रांत की जातियों का ब्यौरा देती है। लेकिन अंग्रेजों ने भी आम तौर पर भारतीय परंपराओं खासकर वर्ण व्यवस्था को कम ही छेड़ा।
मैकाले उन चंद अंग्रेज अफसरों में थे, जिन्होंने जाति व्यवस्था और उससे जुड़े भेदभाव पर हमला बोला। समान अपराध के लिए सभी जातियों के लोग समान दंड के भागी बनें, इसके लिए नियम बनाना एक युगांतकारी बात थी। पहले लॉ कमीशन की अध्यक्षता करते हुए मैकाल जो इंडियन पीनल कोड बनाया, उसमें पहली बार ये बात तय हुई कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं और अलग अलग जातियों को एक ही अपराध के लिए अलग अलग दंड नहीं दिया जाएगा। शिक्षा को सभी जाति समूहों के लिए खोलकर और शिक्षा को संस्कृत और फारसी जैसी आभिजात्य भाषाओं के चंगुल में मुक्त करने की पहल कर मैकाले ने भारतीय जाति व्यवस्था पर दूसरा हमला किया।
गुरुकुलों से शिक्षा को बाहर लाने की जो प्रक्रिया मैकाले के समय में तेज हुई, उससे शिक्षा के डेमोक्रेटाइजेशन का सिलसिला शुरू हुआ। अगर आज देश में 50 लाख से ज्यादा (ये संख्या बार बार कोट की जाती है, लेकिन इसके स्रोत को लेकर मैं आश्वस्त नहीं हो, वैसे संख्य़ा को लेकर मुझे संदेह भी नहीं है) दलित मिडिल क्लास परिवार हैं, तो इसकी वजह यही है कि दलितों को भी शिक्षा का अवसर मिला और आंबेडकर की मुहिम और पूना पैक्ट की वजह से देश में आरक्षण की व्यवस्था हुई।
ये शायद सच है कि मैकाले इन्हीं वजहों से आजादी के बाद देश की सत्ता पर काबिज हुई मुख्यधारा की नजरों में एक अपराधी थे। भारतीय संस्कृति पर हमला करने के अपराधी। देश को गुलाम बनाने वालों से भी बड़े अपराधी। हम विदेशी हमलावरों को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हमारी जीवन पद्धति खासकर वर्णव्यवस्था से छेड़छाड़ करने वाला हमारे नफरत की आग में जलेगा।
वीपी सिंह की मिसाल लीजिए। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ किया। उत्तर प्रदेश में डकैत उन्मूलन के नाम पर पिछड़ों पर जुल्म ढाए, राजीव गांधी की क्लीन इमेज को तार तार कर दिया, बोफोर्स में रिश्वतखोरी का पर्दाफाश किया, लेकिन मुख्यधारा उन्हें इस बात के लिए माफ नहीं करेगी कि उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की कोशिश की। हालांकि वीपी सिंह ने ये कदम राजनीतिक मजबूरी की वजह से उठाया था और वो पिछड़ों के हितैषी कभी नहीं रहे फिर भी वीपी सिंह सवर्ण मानस में एक विलेन हैं और पूरी गंगा के पानी से वीपी सिंह को धो दें तो भी उनका ये 'पाप' नहीं धुल सकता। ये चर्चा फिर कभी।
जाहिर है मैकाले को लेकर दो एक्सट्रीम चिंतन हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसके लिए मैकाले की पूजा होनी चाहिए या उनकी तस्वीर को गोली मार देनी चाहिए। इस अतिवाद को छोड़कर देखें तो मैकाले के समय का द्वंद्व नए और पुराने के बीच, प्राच्य और पाश्चात्य के बीच का था। मैकाले उस द्वंद्व में नए के साथ थे, पाश्चत्य के साथ थे। अंग्रेजी शिक्षा के लिए उनके दिए गए तर्क उनके समग्र चिंतन से अलग नहीं है। इसलिए ये मानने का कोई आधार नहीं है कि मैकाले ने साजिश करके भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली। उनका मिनिट ऑन एजुकेशन (1835) पढ़ जाए। भारत के प्रति मैकाले में न प्रेम है न घृणा। एक शासक का मैनेजेरियल दिमाग है, जो अपनी मान्यताओं के हिसाब से शासन करने के अपने तरीके को जस्टिफाई कर रहा है।
मैकाले की इस बात के लिए प्रशंसा करना विवाद का विषय है कि उनकी वजह से देश में अंग्रेजी शिक्षा आई और भारत आज आईटी सेक्टर की महाशक्ति इसी वजह से बना हुआ है और इसी ज्ञान की वजह से देश में बीपीओ इंडस्ट्री फल फूल रही है। चीन में मैकाले जैसा कई नहीं गया। चीन के लोगों ने अंग्रेजी को अपनाने में काफी देरी की, फिर भी चीन की अर्थव्यवस्था भारत से कई गुना बड़ी है। लेकिन चीन का आर्थिक और सामाजिक परवेश हमसे अलग है और ये तुलना असमान स्थितियों के बीच की जा रही है और भाषा का आर्थिक विकास में योगदान निर्णायक भी नहीं माना जा सकता।
- दिलीप मंडल
बादर गरजे चहुंओर, बिजुरी चमके चारों ओर
हमारे गांव के किनारे से एक नदी बहती है। बागमती। कई बार हमने उसके ओर-छोर की खोज की और ज्यादा से ज्यादा एक बांध के ओर-छोर को ही जान पाये। नदी किनारे एक मंदिर और डोम के दो-चार घर की याद है। एक डोमिन थी, जो बांस के सामान घर में दे जाती थी। उसका चेहरा हमारी मां से मिलता था। एक बार बाढ़ की रिपोर्टिंग करने पटना से गांव गया, तो डोमिन एक तंबू तान कर बांध पर रह रही थी। हम शहर के स्टूडियो से भाड़े का कैमरामैन लेकर पहुंचे थे। उस डोमिन की तस्वीर अख़बार में छपी, जिसे शायद वह नहीं देख पायी होगी। अख़बार का सर्कुलेशन उतना नहीं था, जो बाढ़ विस्थापितों से भरे बांध तक पहुंच पाता।
सावन में बाढ़ आती थी। सावन में ही कांवरियों की टोली बाबाधाम के लिए निकलती थी और फूल गये पांव में पट्टी बांध कर लौटती थी। हमारे घर चिउड़ा, इलायची दाना और पेड़े का एक टुकड़ा आता था। साथ में केसरिया रंग की बद्धी भी आती थी, जिसे गले में लटकाये हमारा बचपन बीता है। प्रगतिशीलता की ऐसी पहली बयार कभी नहीं बही कि हम उसे उठा कर खिड़की के बाहर फेंकते।
सन 99 के सावन में मेरी मां मरी। बांध के पार बाढ़ थी, इसलिए हमारी आम गाछी में उसे जलाया गया। एक पेड़ को काटकर चिता बनायी गयी। मेरा हाथ पकड़कर उस चिता में चारों दिशाओं से किसी आग दिलवायी और वो धू-धू करके जल उठी। कई लोग सावन में मरते हैं और सुना है जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलती। मिल भी जाती है, तो जलने में मुश्किल होती है। रिवाज ये है कि जब तक चिता पूरी न जले, कठिहारी (हमारे यहां का शब्द है लाश के साथ श्मशान गये लोगों के लिए) में गये लोग वापिस नहीं लौटते।
सावन में हमने कम लोगों को सुखी देखा है। एक बार गांव के अपने दोस्त भाई के साथ किसी बीयर बार में शाम बिता कर हम शहर में ख़ूब भीगे और सखी-सहेलियों के बारे में बातें करते रह गये। शहर से गांव पैदल लौटे। वो बेहतर गवैया है और होली में उसके रहने से गांव में रौनक रहती है। वो पिछले कई सालों से गांव जा रहा है और मैं पिछले कई सालों से गांव नहीं गया हूं। आजकल वो आईसीआईसीआई बैंक के लखनऊ ब्रांच में अफसर है और उसने कार भी ख़रीद ली है। मेरी ही तरह फैल गया है और कोई बता रहा था, इस साल जो होली बीती, उसमें वह अपनी कार से गांव गया था।
मैथिली के एक नाटककार हैं महेंद्र मलंगिया। उनका एक नाटक है - ओकरा आंगनक बारहमासा। बारह महीने के दुखी-दारुण जीवन की दिल को बेधने वाली कारुणिक कथा है। उसमें सावन का एक रुलाने वाला राग है। वरना सावन के सुख में भीगे गीतों को ही हम जानते हैं। सावन में ही कजरी गायी जाती है और अक्सर विरह के सुर में होती है। हम ज़िंदगी की बेहतरीन सुबहों में अपनी बुआओं से कजरी सुनते आये हैं। बाद में रेडियो स्टेशन से कजरी के कई अंदाज़ हमारे हिस्से आये। पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी की आवाज़ में कजरी सुनी। शुभा मुदगल और शोभा गुर्टू ने भी कजरी गायी हैं।
लेकिन जो कजरी हमने छन्नूलाल मिश्रा की आवाज़ में सुनी है, उसका कोई जवाब नहीं है। बनारसी फकीरी वाली आवाज़। गंगाघाटों पर आवारा उड़ते हुए कुछ खोजती-सी। पान की खस-खस से भरी हुई। दीवाना बनाने के लिए सबसे निर्गुण आवाज़। ऐसी आवाज़ इस धरती पर अकेली है। सुनिए, उनकी आवाज़ में ये बेमिसाल बनारसी कजरी,
Saturday, December 22, 2007
उस्ताद फ़तेह अली ख़ान और यान गार्बारेक की जुगलबन्दी
 पटियाला घराने के अग्रगण्य गायकों में थे अमानत अली खान और फ़तेह अली ख़ान बन्धु . बड़े यानी अमानत अली ख़ान साहब अब नहीं हैं. खयाल गायकी में इन दोनों का बड़ा नाम रहा है.
पटियाला घराने के अग्रगण्य गायकों में थे अमानत अली खान और फ़तेह अली ख़ान बन्धु . बड़े यानी अमानत अली ख़ान साहब अब नहीं हैं. खयाल गायकी में इन दोनों का बड़ा नाम रहा है.  यान गार्बारेक नार्वे के मशहूर सैक्सोफ़ोन वादक हैं और पिछले कुछ दशकों से उन्होंने दुनिया भर के संगीतकारों के साथ संगत और जुगलबन्दी की है. वे अपनी प्रयोगधर्मिता के लिये जाने जाते हैं. इन्होने स्कैंडिनेविया की लोकधुनों पर काम किया है और शेक्सपीयर के नाटकों का संगीत भी दिया है. अज़ान की धुन पर उनका काम उल्लेखनीय रहा है. भारतीय संगीत से गहरे प्रभावित गार्बारेक ने उस्ताद शौकत अली ख़ान और उस्ताद नाज़िम अली ख़ान के साथ भी काम किया है.
यान गार्बारेक नार्वे के मशहूर सैक्सोफ़ोन वादक हैं और पिछले कुछ दशकों से उन्होंने दुनिया भर के संगीतकारों के साथ संगत और जुगलबन्दी की है. वे अपनी प्रयोगधर्मिता के लिये जाने जाते हैं. इन्होने स्कैंडिनेविया की लोकधुनों पर काम किया है और शेक्सपीयर के नाटकों का संगीत भी दिया है. अज़ान की धुन पर उनका काम उल्लेखनीय रहा है. भारतीय संगीत से गहरे प्रभावित गार्बारेक ने उस्ताद शौकत अली ख़ान और उस्ताद नाज़िम अली ख़ान के साथ भी काम किया है.'रागाज़ एंड सागाज़' नामक उन का जुगलबन्दी का अल्बम उस्ताद फ़तेह अली खान के साथ १९९२ में रिलीज़ हुआ था. उसी में से सुनिये एक कम्पोज़ीशन
(१२ मिनट ५२ सेकेन्ड)
Friday, December 21, 2007
स्मृतियों के एकांत संगीत में गोविन्द बल्लभ पंत की स्मृति और शमशेर की एक कविता
गोविन्द बल्लभ पंत ने अठारह-उन्नीस उम्र से काव्य रचना आरंभ की। उनकी ख्याति मुख्यत: नाटककार और कथाकार के रूप में रही है। उनके नाटकों में 'कंजूस की खोपडी','राजमुकुट','वरमाला','अंत:पुर का छिद्र','अंगूर की बेटी','सुहाग बिन्दी','ययाति' आदि प्रमुख हैं। उन्होंने कई नाटक कंपनियों -व्याकुल भारत, राम विजय, न्यू एल्फ्रेड,पृथ्वी थिएटर्स आदि के लिए नाटक लिखे और अभिनय भी किया। ऐसे नाटकों में 'अहंकार','प्रेमयोगी','मातृभूमि','द्रौपदी स्वयंवर'प्रमुख हैं। पंत जी ने जीवन और जगत के विविध अनुभवों पर कई उपन्यासों की रचना की है जिनमें 'प्रतिमा','मदारी','तारिका','अमिताभ','नूरजहां','मुक्ति के बंधन','फॉरगेट मी नाट','मैत्रेय','यामिनी'आदि चर्चित रहे हैं। उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाओं में'विषकन्या'( एकांकी संग्रह) तथा 'एकादशी' और 'प्रदीप'(दोनों कहानी संग्रह) शामिल हैं। उन्होंने लगभग ७५ वर्षों तक लेखन किया लेकिन १९६० के बाद से वे एक रचनाकार के रूप में चुप ही रहे। अगर उनकी यह चुप्पी टूटती तो संभवत: पुस्तकों की संख्या की दृष्टि से वे महापंडित राहुल सांकृत्यायन के निकट पहुंच जाते।
मई-जून १९८८ में मैने पहली बार पंत जी को देखा-पहचाना जबकि कफी लंबे समय से नगर की साहित्यिक-सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हुए भी यह सुनता भर था कि प्रख्यात साहित्यकार गोविन्द बल्लभ पंत मेरे छात्रावास ब्रुकहिल के आसपास ही कहीं रहते हैं लेकिन उनसे मिलने का प्रयास कभी नहीं किया था पता नहीं वह कौन सी हिचक थी जो रोके रखती थी जबकि अन्य नये-पुराने साहित्यकारों के नैनीताल में होने की खबर मेरे जैसे नौसिखिये कलमघिस्सुओं में जोश भर देती थी और हम उनसे मिलते भी थे १९८८ की गर्मियों में शमशेर बहादुर सिंह् नैनीताल में थेइस मौके पर 'पहाड़' और 'नैनीताल समाचार ने 'एक शाम शमशेर के नाम' काव्य गोष्ठी का आयोजन कियाप्रोफेसर शेखर पाठक ने मुझे यह काम सौंपा कि कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिये गोविन्द बल्लभ पंत जी से बात हो गई है और मैं उन्हें आयोजन स्थल सी.आर.एस.टी.इंटर कालेज तक लिवा लाऊंतब मैनें पहली बार जाना कि पंत जी के पुत्र कृषि या ऐसे ही किसी विभाग में बड़े अफसर हैं और पंत जी उन्हीं के साथ ओक पार्क में रहते हैं
खैर, नियत तारीख और समय पर मैं पंत जी के निवास पर पहुंचादरवाजा उनकी पुत्रवधु ने खोला ,मैंने अप्ना मंतव्य बताया तो उन्होने बैठने के लिये कहामैंने ध्यान दिया एक सुरुचि संपन्न बैठक,सोफे पर बैठा एक वृद्ध व्यक्ति-भूरे रंग की लंबी कमीज और सफेद पायजामा पहनेऐसा लगा इनको कहीं देखा है.. प्रणाम किया तो उन्होंने हाथ जोड़कर उत्तर दिया वे साहित्यकार गोविन्द बल्लभ पंत थे'ऐसा क्या खास है इस मनुष्य में...'मैंने गौर करना चाहाअरे! इन्हें तो अक्सर अपने छात्रावास के सामने वाली सड़क पर घूमते-टहलते देखा हैक़्या यह वही मनुष्य है जो अपने युग का चमकता हुआ सितारा था;अपने जमाने का मशहूर कथाकार और नाटककार क़्या यह वही मनुष्य है जो पं.राधेश्याम कथावाचक और पृथ्वीराज कपूर जैसी महान हस्तियों के साथ काम कर चुका है इतना ही नहीं असहयोग आंदोलन का दमदार सिपाही और एक लोकप्रिय शिक्षक भी रहा है...मुझे शर्म आई कि तब तक एकाध छिटपुट कहानियों के अतिरिक्त मैंने उनकी कोई भी किताब नहीं पढी थी,यहां तक कि बी.ए.के कोर्स में उनका नाटक 'पन्ना'शामिल था परंतु हमने उसका विकल्प 'लहरों के राजहंस'(मोहन राकेश)ही पढा था
पंत जी कार्यक्रम में आएशायद कई दशकों बाद उनकी और शमशेर जी की यह प्रत्यक्ष मुलाकात थीशमशेर जी कुछ-कुछ पूछते रहे और पंत जी चुपशमशेर जी ने अपनी दो-तीन कविताओं का पाठ किया और थक गयेडा.रंजना अरगड़े ने उनकी कुछ कवितायें पढीं, कुछ और लोगों ने भी कविता पाठ किया त्रिनेत्र जोशी अपने कैमरे से सचल और अचल तस्वीरें उतारते रहेपंत जी चुप मुस्कुराते रहेशमशेर जी का भी यही हाल थाहम सबके लिए यह एक साथ एक मंच पर 'दो सितारों के मिलन' का एक ऐसा अद्भुत क्षण था जो दोबारा लौटकर नहीं आने वाला थाकार्यक्रम सफल रहा इसके बाद लगभग दो साल तक मैं प्रायः रोज ही पंत जी को छड़ी थामे सड़क पर टहलते हुये देखता रहाकभी सामने पड़ जाने पर प्रणाम भी करता और वह कुछ पहचानने की कोशिश करते हुए आगे बढ जातेमन करता था कि उनके साथ चलूं,ढेर सारी बातें पूछूं,ढेर सारी बातें सुनूं लेकिन वे इतने चुप-चुप रहते थे कि उनके एकांत संगीत की लय में खलल डालने की हिम्मत नहीं होती थीवक्त गुजरता रहा और मैं पंत जी को दूर से देखते हुए उनके साहित्य के निकट आता रहा
अंततः एक दिन मेरी पढाई पूरी हुई और सरोवर नगरी से प्रत्यक्ष नाता टूटाइस बीच देश-दुनिया में बहुत कुछ बना,बिगड़ा,बदलाइस बीच कई साहित्यकरों क निधन हुआ और पत्र-पत्रिकाओं ,रेडियो- टी.वी.पर उनको खूब याद किया गया यह जरूरी भी था और जायज भी लेकिन उस वक्त जब गोविन्द बल्लभ पंत का निधन हुआ था तब उनके स्मरण को लेकर जो ठंडापन व्याप्त हुआ था वह आज तक दिखाई देता है-अनुभव होता हैऐसा ठंडापन क्या यह प्रदर्शित-प्रकट नहीं करता है कि आज की दुनिया में आप तभी तक महान हैं जब तक कि मंच पर हैं और मुखर हैं
शमशेरबहादुर सिंह की कविताः महुवा
यह अजब पेड़ है जिसमें कि जनाब
इस कदर जल्द कली फूटती है
कि अभी कल देखो
मार पतझड़ ही पतझड़ था इसके नीचे
और अब
सुर्ख दिये,सुर्ख दियों का झुरमुट
नन्हें-नन्हें,कोमल
नीचे से ऊपर तक -
झिलमिलाहट का तनोबा मानो-
छाया हुआ हैयह अजब पेड़ है
पत्ते कलियां
कत्थई पान का चटक रंग लिये -
इक हंसी की तस्वीर -
(खिलखिलाहट से मगर कम- दर्जे)
मेरी आंखों में थिरक उठती है
मुझको मालूम है ,ये रंग अभी छूटेंगे
गुच्छे के गुच्छे मेरे सर पै हरी
छतरियां तानेंगेः गुच्छे के गुच्छे ये
फिर भी,फिर भी, फिर भी
एक बार और भी फिर भी शाम की घनघोर घटायें
-आग-सी लगी हो जैसे हर -सू-
सर पै छा जाएँगी :
कोई चिल्ला के पुकारेगा ,कि देखो,देखो
यही महुवे का महावन है !
भारतीय समाज का दा विंची कोड!
उस निमंत्रण पत्र की कुछ पंक्तियां यहां रख रहा हूं। पार्टी में मैं जा नहीं पाया, इसलिए वहां क्या हुआ, इसका ब्यौरा देना संभव नहीं है। आप भी पढ़िए और चौंकने के लिए तैयार हो जाइए -
मैकाले शायद पहला शख्स था जिसने भारत के स्वतंत्र होने की कल्पना की थी। मैकाले का 10 जुलाई, 1833 को ब्रिटिश संसद में दिया गया भाषण देखिए - "भारत के लोग कुशासन में रहें और हमारे गुलाम रहें, इससे बेहतर है कि वो आजाद हों और अपना शासन अच्छे से चलाएं।"
इसी भाषण में मैकाले कहते हैं- "हमें कहा जाता है कि ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब भारतीय लोग सिविल और मिलिट्री सर्विस में ऊंचे पदों पर आसीन होंगे। मैं इस सोच का कड़ा प्रतिवाद करता हूं।"
रंग में भारतीय पर विचार में अंग्रेज वाला बार बार दोहराया जाने वाला पूरा कोट इस तरह है-
“"In point, I fully agree with the gentlemen to whose general views I am opposed to. I feel with them that it is impossible for us, with our limited means, to attempt to educate the body of the people. We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect. To that class we may leave it to refine the vernacular dialects of the country, to enrich those dialects with terms of science borrowed from the Western nomenclature, and to render them by degrees fit vehicles for conveying knowledge to the great mass of the population”.
भारतीय इतिहास की हर किताब में इस कोटेशन की पहली और आखिरी लाइन का जिक्र नहीं होता। पहली लाइन में इस बयान का संदर्भ है कि "जब तक हम भारत के सभी लोगों को शिक्षा दे पाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं" जबकि आखिरी लाइन में बताया गया है कि किस तरह भारतीय भाषाओं में पश्चिमी शब्दावलियों का समावेश किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ज्ञान पहुंचाया जा सके।
भारतीय और अरबी साहित्य को नीचे दर्जे का मानने वाले मैकाले अपने देश के पुराने साहित्य के बारे में भी अच्छी राय नहीं रखते थे। इसलिए इस बारे में उनका विचार नस्लीय भेदभाव से कहीं ज्यादा नवीन और प्राचीन के टकराव का नतीजा है।
मैकाले का भारत पर दो कारणों से निर्णायक असर हुआ है। पहला तो शिक्षा के क्षेत्र में उनके विचारों को अंग्रेजी सरकार ने माना और देश में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम को मान्यता मिली। उनका दूसरा योगदान देश में आईपीसी और सीआरपीसी लागू करने की दिशा में था, जिसकी वजह से लगभग कई हजार साल बाद भारत में अलग अलग जाति के द्वारा किए गए समान अपराध के लिए समान दंड के कानून का चलन शुरू हुआ।
(मेरी टिप्पणी- मैकाले से नफरत करने के बावजूद भारत में आज भी ये दो चीजें बदली नहीं हैं।)
1933 के उसी भाषण के ये अंश देखिए।
"…सबसे बुरी व्यवस्था वो है जिसमें ब्राह्मणों के लिए हल्के दंड का प्रावधान है क्योंकि वो सृष्टिकर्ता के मुंह से उत्पन्न हुए हैं। जबकि पैरों से उत्पन्न शूद्रों के लिए कड़े दंड का प्रावधान हैं। जाति विभेद और भेदभाव के कारण भारत का काफी नुकसान हो चुका है।"
हिंदू धर्म और शिक्षा के बारे में मैकाले प्राच्यविदों को जवाब देते हैं -
" (आपकी बात मानें तो) हमें उन्हें गलत इतहास, गलत खगोलशास्त्र, गलत चिकित्साशास्त्र पढ़ाना होगा क्योंकि गलत बातें सिखाने वाला धर्म इनसे जुड़ा है... भारतीय युवकों को ये सिखाना उनका समय नष्ट करना होगा कि गधे को छूने के कैसे खुद के पवित्र करें और बकरी मारने के पाप से मुक्त कैसे मिलेगी।"
इस निमंत्रण पत्र के मुताबिक क्लाइव ने हिंदुस्तानियों को हराकर उन्हें गुलाम बनाया, ये बात हिंदू मुख्यधारा (सवर्ण चिंतन) बर्दास्त कर सकती है, करती है। इसलिए क्लाइव से नफरत करने की बात हमें नहीं सिखाई जाती। लेकिन भारतीय संस्कृति, जातिव्यवस्था, शिक्षा प्रणाली और धर्म को चुनौती देने वाला मैकाले को बर्दास्त कैसे किया जा सकता है?
(मेरी टिप्पणी)
एक सवाल है आपसे। आज कल्पना कीजिए अगर ब्रिटिश संसद की उस बहस में मैकाले की हार हो गई होती और प्राच्यविद जीत गए होते। उस आधुनिक भारत कि कल्पना कीजिए जहां के सभी विश्वविद्यालयों और इंस्टिट्यूट में संस्कृत और फारसी और ऊर्दू में पढ़ाई हो रही हो। और कल्पना कीजिए उस भारत की जहां एक ही अपराध के लिए ब्राहा्ण, क्षत्रीय, वैश्य और शूद्र अलग-अलग सजाएं भुगत रहे होते।
यानी इस मैकाले में अभी बहुत जान है! कई सवाल खड़े करता है ये मसला। बहस में बने रहिए हमारे साथ। आगे इस निमंत्रण पत्र में लिखी बातों की सच्चाई जानेंगे और उस कोड को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम आधुनिक भारतीय इतिहास है। अभी किसी फैसले पर मत पहुंचिए। मानस खुला रखिए और हो सके तो किसी कोने में पड़ी इतिहास की किताबों की धूल झाड़िए। क्योंकि हमारे ही देश के कुछ लोग मैकाले की तस्वीर को जूते नहीं मार रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं।
तो दोस्त, सतरंगी भारतीय समाज जितने जवाब देता है उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़े करता है। हम सभी भाग्यशाली है कि इतने रोचक और तेजी से बदलते समय को देख पा रहे हैं। जारी रहेगी ये चर्चा।
ब्लागिंग के दस साल

ये हैं जोर्न बार्जर। १७ दिसम्बर १९९७ को अपनी व्यक्तिगत टिप्पणियों को इन्टरनेट पर जगह देने के उद्देश्य से इन्होंने logging the web को मिलाकर 'ब्लाग' शब्द की रचना की। उसके कुछ महीनों तक ब्लागों की संख्या फ़क़त दहाई का आंकड़ा छू पाई।
लेकिन सूचना तक्नीकी के भीषण प्रसार के बाद यह संख्या लगातार बढ़ती गई है। इस साल अप्रैल में छपी “State of the Live Web” रिपोर्ट के मुताबिक ब्लागरों की संख्या सात करोड़ बीस लाख से ऊपर पहुंच गई थी। अप्रैल २००६ में यह संख्या तीन करोड़ पचास लाख थी जबकि २००५ में करीब अस्सी लाख।
ब्लागिंग को आसान बनाने के लिये नित नए नए उपकरणों के आते जाने से यह आसान और बहुत सुग्राह्य बन गई है। एक मोटे अनुमान के हिसाब से रोज़ करीब पन्द्रह लाख पोस्ट चढ़ाई जाती हैं। यूरोप और अमेरीका में इस ट्रैंड के अगले साल तक धीमे पड़ जाने का क़यास लगाया जा रहा है।
इस के उलट हिन्दी में यह ट्रैंड लगातार बढ़ता जाएगा, इस बात से कौन इन्कार कर सकता है। देर आयद दुरुस्त आयद।
(अधिकतर सूचनाओं के लिए http://arstechnica.com/ का आभार)
*Wordweb Dictionary के अनुसार ब्लाग की परिभाषा: A shared on-line journal where people can post diary entries about their personal experiences and hobbies.
हमारी गालियों में मैकाले है, क्लाइव नहीं
कौन था क्लाइव
क्लाइव न होता तो क्या भारत में कभी अंग्रेजी राज होता? इतिहास का चक्र पीछे लौटकर तो नहीं जाता इसलिए इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता। लेकिन इतिहास हमें ये जरूर बताता है कि क्लाइव के लगभग एक हजार यूरोपीय और दो हजार हिंदुस्तानी सिपाहयों ने पलासी की निर्णायक लड़ाई (22 जून, 1757) में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा कर भारत में अंग्रेजी राज की नींव रखी थी। वो लड़ाई भी क्या थी? सेनानायक मीरजाफर ने इस बात का बंदोबस्त कर दिया था कि नवाब की ज्यादातर फौज लड़ाई के मैदान से दूर ही रहे। एक दिन भी नहीं लगे थे उस युद्ध में। उस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारतीय संपदा की लूट का जो सिलसिला शुरू किया, उसकी बराबरी दक्षिण अमेरिका में स्पेन के युद्ध सरदारों की मचाई लूट से ही की जा सकती है।
और कौन था मैकाले
मैकाले को भारतीय इतिहास का हर छात्र एक ऐसे शख्स के रूप में जानता है जिसने देश को तो नहीं लेकिन भारतीय मानस को जरूर गुलाम बनाया। हमारी सामूहिक स्मृति में इसका असर इस रूप में है कि हम जिसे विदेशी मिजाज का, देश की परंपरा से प्रेम न करने वाला, विदेशी संस्कृति से ओतप्रोत मानते हैं उसे मैकाले पुत्र, मैकाले की औलाद, मैकाले का मानस पुत्र, मैकाले की संतान आदि कहकर गाली देते हैं।
लेकिन भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक क्लाइव को लेकर हमारे यहां घृणा का ऐसा भाव आश्चर्यजनक रूप से नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है। मैकाले जब भारत आया तो भारत में अंग्रेजी राज जड़ें जमा चुका था। मैकाले को इस बात के लिए भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है कि उसने क्लाइव की तरह तलवार और बंदूक के बल पर एक देश को गुलाम बनाया। या कि उसने छल से बंगाल के नवाब को हरा दिया। मैकाले अपने हाथ में तलवार नहीं कलम लेकर भारत आया था।
लेकिन मैकाले फिर भी बड़ा विलेन है।
मैकाले हमारी सामूहिक स्मृति में घृणा का पात्र है तो ये अकारण नहीं है। मैकाले के कुछ चर्चित उद्धरणों को देखें। उसका दंभ तो देखिए
"मुझे एक भी प्राच्यविद (ओरिएंटलिस्ट) ऐसा नहीं मिला जिसे इस बात से इनकार हो कि किसी अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी की किताबों का एक रैक पूरे भारत और अरब के समग्र साहित्य के बराबर न हो।"
और उनके इस कथन को कौन भूल सकता है। प्रोफेसर बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी की इतिहास की किताब में देखिए।
" फिलहाल हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारे और हम जिन लाखों लोगों पर राज कर रहे हैं, उनके बीच इंटरप्रेटर यानी दुभाषिए का काम करे। लोगों का एक ऐसा वर्ग जो खून और रंग के लिहाज से भारतीय हो, लेकिन जो अभिरूचि में, विचार में, मान्यताओं में और विद्या-बुद्धि में अंग्रेज हो।"
इतिहासकार सुमित सरकार मैकाले को कोट करते हैं-
"अंग्रेजी में शिक्षित एक पढ़ा लिखा वर्ग, रंग में भूरा लेकिन सोचने समझने और अभिरुचियों में अंग्रेज।"
भारतीय इतिहास की किताबों में मैकाले इसी रूप में आते हैं। पांचजन्य के एक लेख में मैकाले इस शक्ल में आते हैं-
लार्ड मैकाले का मानना था कि जब तक संस्कृति और भाषा के स्तर पर गुलाम नहीं बनाया जाएगा, भारतवर्ष को हमेशा के लिए या पूरी तरह, गुलाम बनाना संभव नहीं होगा। लार्ड मैकाले की सोच थी कि हिंदुस्तानियों को अँग्रेज़ी भाषा के माध्यम से ही सही और व्यापक अर्थों में गुलाम बनाया जा सकता है। अंग्रेज़ी जानने वालों को नौकरी में प्रोत्साहन देने की लार्ड मैकाले की पहल के परिणामस्वरूप काँग्रेसियों के बीच में अंग्रेज़ी परस्त काँग्रेसी नेता पं. जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एकजुट हो गए कि अंग्रेज़ी को शासन की भाषा से हटाना नहीं है अन्यथा वर्चस्व जाता रहेगा और देश को अंग्रेज़ी की ही शैली में शासित करने की योजनाएँ भी सफल नहीं हो पाएँगी।...भाषा के सवाल को लेकर लार्ड मैकाले भी स्वप्नदर्शी थे, लेकिन उद्देश्य था, अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से गुलाम बनाना।
तो ऐसे मैकाले से भारत नफरत न करे तो क्या करे? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, दोस्त।
Thursday, December 20, 2007
वो बात सारे फ़साने में जिसका ज़िक्र न था, वो बात उन को बहुत नागवार गुज़री है

तलाश में है सहर, बार बार गुज़री है
** तस्वीर फ़ैज़ साहब की है (http://www.faiz.com/ से साभार)
क्लाइव या मैकाले - किसे पहले जूते मारेंगे आप?
इन दो तस्वीरों को देखिए। इनमें ऊपर वाले हैं लार्ड क्वाइव और नीचे हैं लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड वो ब्रिटेन में होंगे हम उन्हें आगे क्लाइव और मैकाले कहेंगे। एक सवाल पूछिए अपने आप से। कभी आपको अगरह कहा जाए कि इनमें से किसी एक तस्वीर को जूते मारो, या पत्थर मारो या
अनुरोध इतना है कि इस सवाल को देखकर किसी नए संदर्भ की तलाश में नेट पर या किताबों के बीच न चले जाइएगा। अपनी स्मृति पर भरोसा करें, जो स्कूलों से लेकर कॉलेज और अखबारों से लेकर पत्रिकाओं में पढ़ा है उसे याद करें। और जवाब दें। ये सवाल आपको एक ऐसी यात्रा की ओर ले जाएगा, जिसकी चर्चा कम हुई है। जो इन विषयों के शोधार्थी, जानने वाले हैं, उनके लिए मुमकिन है कि ये चर्चा निरर्थक हो। लेकिन इस विषय पर मैं अभी जगा हूं, इसलिए मेरा सबेरा तो अभी ही हुआ है। इस पर चर्चा आगे जारी रहेगी।
Wednesday, December 19, 2007
दुनिया भर के बहते हुए खून और पसीने में हमारा भी हिस्सा होना चाहिऐ
हिस्सा
बह रहे पसीने में जो पानी है वह सूख जाएगा
लेकिन उस में कुछ नमक भी है
जो बच रहेगा
टपक रहे खून में जो पानी है वह सूख जाएगा
लेकिन उस में कुछ लोहा भी है
जो बच रहेगा
एक दिन नमक और लोहे की कमी का शिकार
तुम पाओगे खुद को और ढेर सारा
खरीद भी लोगे
लेकिन तब पाओगे कि अरे
हमें तो अब पानी भी रास नहीं आता
तब याद आएगा वह पानी जो
तुम्हारे देखते-देखते नमक और लोहे का
साथ छोड़ गया था
दुनिया के नमक और लोहे में हमारा भी हिस्सा है
तो फिर दुनिया भर के बहते हुए खून और पसीने में
हमारा भी हिस्सा होना चाहिऐ
लोहे की रेलिंग
थोडी सी आक्सीजन और थोडी सी नमी
वह छीन लेटी है हवा से
और पेंट की परत के नीचे छिप कर
एक खुफिया कारर्वाई की शुरुआत करती है
एक दिन अचानक
एक पपडी छिलके - सी उतरती है
और चुटकी भर भुरभुरा लाल चूरा
चुपके से धरती की तरफ
लगाता है छलाँग
(गुरुत्वाकर्षण इस में उसकी मदद करता है)
यह शिल्प और तकनीक के जब्दों से
छूटकर आज़ाद होने की
जी तोड़ कोशिश
यह घर लौटने की एक मासूम इच्छा
आखिर थोडी सी आक्सीजन और
थोडी सी नमी
तो हमें भी ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए
बस थोडी सी आक्सीजन
और थोडी सी नमी
वह भी छीन लेती है हवा से।
पार
पुल पार करने से
पुल पार होता है
नदी पार नहीं होती
नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना
नदी में धंसे बिना
पुल का अर्थ भी समझ में नहीं आता
नदी में धंसे बिना
पुल पार करने से
पुल पार नहीं होता
सिर्फ़ लोहा-लंगड़ पार होता है
कुछ भी नहीं होता पार
नदी में धंसे बिना
न पुल पार होता है
न नदी पार होती है
कुछ लोग
कुछ लोग पांवों से नहीं
दिमाग से चलते हैं
ये लोग
जूते तलाशते हैं
अपने दिमाग के नाप के।
समुद्र पर हो रही है बारिश
क्या करे समुद्र
क्या करे इतने सारे नमक का
कितनी नदियां आईं और कहां खो गईं
क्य पता
कितनी भाप बनाकर उड़ा दीं
इसका भी कोई हिसाब उसके पास नहीं
फ़िर भी संसार की सारी नदियां
धरती का सारा नमक लिये
उसी की तरफ़ दौड़ी चली आ रही हैं
तो क्या करे
कैसे पुकारे
मीठे पानी में रहने वाली मछलियों को
प्यासों को क्या मुंह दिखाए
कहां जाकर डूब मरे
खुद अपने आप पर बरस रहा है समुद्र
समुद्र पर हो रही है बारिश
नमक किसे नहीं चाहिये
लेकिन सबकी ज़रूरत का नमक वह
अकेला क्यों ढोए
क्या गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध
उस के उछाल की सज़ा है यह
या धरती से तीन गुना होने की प्रतिक्रिया
कोई नहीं जानता
उसकी प्राचीन स्मृतियों में नमक है या नहीं
नमक नहीं है उसके स्वप्न में
मुझे पता है
मैं बचपन से उसकी एक चम्मच चीनी
की इच्छा के बारे में सोचता हूं
पछाड़ें खा रहा है
मेरे तीन चौथाई शरीर में समुद्र
अभी - अभी बादल
अभी - अभी बर्फ़
अभी -अभी बर्फ़
अभी - अभी बादल।
सीढ़ी
मुझे एक सीढ़ी की तलाश है
सीढ़ी दीवार पर चढ़ने के लिए नहीं
बल्कि नींव में उतरने के लिए
मैं क़िले को जीतना नहीं
उसे ध्वस्त कर देना चाहता हूं।
दीमकें
दीमकों को
पढ़ना नहीं आता
वे चाट जाती हैं
पूरी
किताब।
छ्ह दिसम्बर
इतिहास के बहुत से भ्रमों में से
एक यह भी है
कि महमूद गज़नवी लौट गया था
लौटा नहीं था वह
यहीं था
सैकड़ों बरस बाद अचानक
वह प्रकट हुआ अयोध्या में
सोमनाथ में उसने किया था
अल्लाह का काम तमाम
इस बार उस का नारा था
जय श्रीराम ।
Tuesday, December 18, 2007
बधाई
निरभय निरगुन गुन रे गाऊँगा
निरभय निरगुन गुन रे गाऊँगा ।
मूल कमल दृढ आसन बांधूं जी, उलटी पवन चढाऊंगा ॥
मन ममता को थिर कर लाऊं जी, पाँचों तत्व मिलाऊँगा ॥
इंगला, पिंगला, सुखमन नाड़ी जी, तिरवेनी पर हौं न्हाऊंगा ॥
पांच पचीसों पकड़ मंगाऊं जी, एक ही डोर लगाऊँगा ॥
शून्य शिखर पर अनहद बाजे जी, राग छत्तीस सुनाऊँगा ॥
कहत कबीरा सुनो भाई साधो जी, जीत निशान घुराऊँगा ॥
Monday, December 17, 2007
'ब्लॉग ब्लॉग है, और साहित्य साहित्य' उर्फ़ ऎसी भी क्या हड़बड़ी है
हिन्दी कि सबसे बडी बदकिस्मती यही रही है कि लोगों में पढ़ने कि प्रवृत्ति धीरे धीरे लुप्त होती गयी है। माना कि हिन्दी के बड़े प्रकाशक अच्छी किताबों कि इतनी कम प्रतियां छापते हैं (चालीस करोड़ भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली हिन्दी के किसी 'बैस्टसेलर' की आज कल अमूमन ६०० कापी छपती हैं) कि लोगों तक उनका पहुँचना मुहाल होता है। लेकिन हिन्दी को बचाने का कार्य छोटे छोटे कस्बों से निकलने वाली पत्रिकाओं ने लगातार अपने स्तर पर जारी रखा है। इस समय हिन्दी में जितनी लघु पत्रिकाएँ निकल रही हैं, उतनी कभी नहीं निकलती थीं (आज के 'अमर उजाला' में मंगलेश डबराल का लेख देखें)। ये इन लघु पत्रिकाओं की देन है कि हिन्दी लेखकों की कई पीढियां एक साथ कार्यरत हैं। और यह कार्य इंटरनेट और ब्लॉग के आने से कई दशक पहले से चल रहा है।
साहित्य का इतिहास उठा कर देखें तो पाएंगे कि पहले केवल कविता थी। उस के बाद गद्य की बारी आयी। एक अरसे तक नाटक ही लिखे जाते रहे। कई सदियों बाद उपन्यास की उत्पत्ति हुई तो उस के लिए भी जगह बनी। फिर कहानियाँ, एकांकी और तमाम विधाएं आती गयीं और उन सब के लिए न सिर्फ जगह बनी, वे लोकप्रिय भी हुईं। जब क्रिस्टोफर मार्लो ने एलिज़ाबेथन समय के शास्त्रीय नाटकों के युग में मुक्त छंद (Blank Verse) का प्रयोग किया तो वह शुरू में लोगों को पचा ही नहीं। लेकिन उस के दस सालों के भीतर 'हैमलेट', 'मैकबेथ', 'किंग लीयर' जैसे नाटक भाषा-देश- भूगोल की सरहदें लाँघ कर अमर हो गए। रिपोर्ताज, यात्रावृत्त, ग़ज़ल, हाईकू, सौनेट ... कितनी कितनी विधाएं हैं।
अब ब्लॉग आया है तो जाहिर है वह भी अपनी जगह बनाएगा ही। लेकिन इस में किसी दूसरे फॉर्मेट से प्रतिद्वंद्विता की क्या ज़रूरत है। ब्लॉग ने मनचाही रचना करने की स्वतंत्रता बख्शी है तो अभी थोडे धैर्य के साथ इस औज़ार के गुण-दोषों को चीन्हे जाने की दरकार भी महसूस होती है।
हम लोगों ने जब कबाड़खाना शुरू किया तो जाहिर है हम ने इसे एक नया खिलौना जान कर काफी शरारतें भी कीं लेकिन धीरे धीरे एक ज़िम्मेदारी का अहसास होना शुरू हुआ और साथ ही नए नए आयाम भी खुले (जो अब भी खुल रहे हैं)। मुझे यकीन है ऐसा ही ब्लागिंग में मसरूफ तमाम मित्रों को भी लगा होगा।
सब से बड़ी चीज़ यह है कि ब्लॉग हमें एक ऐसा प्लेटफार्म मुहैय्या कराता है जहाँ हम अपनी पसन्द/ नापसंद सभी के साथ बाँट सकते हैं। हम अपनी मोहब्बत भी बाँट सकते हैं और नफरत भी। हम विनम्रता बाँट सकते हैं और विनयहीनता भी। हम एक दूसरे का तकनीकी ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं (जैसा कि श्री रवि रतलामी और कई अन्य लोग लगातार करते रहे हैं और जिस के लिए उन का आभार व्यक्त करने को शब्द कम पड़ जाएंगे)
फिलहाल हिन्दी हम सब का सरोकार है और होना ही चाहिऐ। 'निज देश' की उन्नति के लिए 'निज भाषा' की उन्नति की ज़रूरत को भारतेंदु जी एक सदी पहले रेखांकित कर चुके हैं। ब्लॉग ने इस के निमित्त एक अदभुत सुअवसर उपलब्ध कराया है। हिन्दी न सिर्फ अब भी महान अभिव्यक्ति का माध्यम है बल्कि वह ऐसा कर भी रही है।
पढिये साहित्य अकादमी पुरूस्कार से सम्मानित हो चुके, वीरेन डंगवाल के कविता संग्रह 'दुश्चक्र में सृष्टा' की शीर्षक कविता।
दुश्चक्र में सृष्टा
कमाल है तुम्हारी कारीगरी का भगवान,
क्या-क्या बना दिया, बना दिया क्या से क्या!
छिपकली को ही ले लो,
कैसे पुरखों
की बेटी छत पर उल्टा
सरपट भागती छलती तुम्हारे ही बनाए अटूट नियम को।
फिर वे पहाड़!
क्या क्या थपोड़ कर नहीं बनाया गया उन्हें?
और बगैर बिजली के चालू कर दी उनसे जो
नदियाँ, वो?
सूंड हाथी को भी दी और चींटी
को भी एक ही सी कारआमद अपनी-अपनी जगह
हाँ, हाथी की सूंड में दो छेद भी हैं
अलग से शायद शोभा के वास्ते
वर्ना सांस तो कहीं से भी ली जा सकती थी
जैसे मछलियाँ ही ले लेती हैं गलफड़ों से।
अरे, कुत्ते की उस पतली गुलाबी जीभ का ही क्या कहना!
कैसी रसीली और चिकनी टपकदार, सृष्टि के हर
स्वाद की मर्मज्ञ और दुम की तो बात ही अलग
गोया एक अदृश्य पंखे की मूठ
तुम्हारे ही मुखड़े पर झलती हुई।
आदमी बनाया, बनाया अंतड़ियों और रसायनों का क्या ही तंत्रजाल
और उसे दे दिया कैसा अलग सा दिमाग
ऊपर बताई हर चीज़ को आत्मसात करने वाला
पल-भर में ब्रह्माण्ड के आर-पार
और सोया तो बस सोया
सर्दी भर कीचड़ में मेढक सा
हाँ एक अंतहीन सूची है
भगवान तुम्हारे कारनामों की, जो बखानी न जाए
जैसा कि कहा ही जाता है।
यह ज़रूर समझ में नहीं
आता कि फिर क्यों बंद कर दिया
अपना इतना कामयाब
कारखाना? नहीं निकली कोई नदी पिछले चार-पांच सौ सालों से
जहाँ तक मैं जानता हूँ
न बना कोई पहाड़ या समुद्र
एकाध ज्वालामुखी ज़रूर फूटते दिखाई दे जाते हैं कभी-कभार।
बाढ़ेँ तो आयीं खैर भरपूर, काफी भूकंप,
तूफ़ान खून से लबालब हत्याकांड अलबत्ता हुए खूब
खूब अकाल, युद्ध एक से एक तकनीकी चमत्कार
रह गई सिर्फ एक सी भूख, लगभग एक सी फौजी
वर्दियां जैसे
मनुष्य मात्र की एकता प्रमाणित करने के लिए
एक जैसी हुंकार, हाहाकार!
प्रार्थनाग्रृह ज़रूर उठाये गए एक से एक आलीशान!
मगर भीतर चिने हुए रक्त के गारे से
वे खोखले आत्माहीन शिखर-गुम्बद-मीनार
ऊँगली से छूते ही जिन्हें रिस आता है खून!
आखिर यह किनके हाथों सौंप दिया है ईश्वर
तुमने अपना इतना बड़ा कारोबार?
अपना कारखाना बंद कर के
किस घोंसले में जा छिपे हो भगवान?
कौन - सा है वह सातवाँ आसमान?
हे, अरे, अबे, ओ करुणानिधान !!!