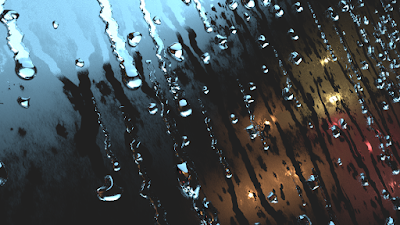‘द हिन्दू’ में 21 अक्टूबर को प्रकाशित लेख का अनुवाद: आशुतोष उपाध्याय
 |
| फ़ोटो: इन्डियन एक्सप्रेस से साभार |
पांच सौ अक्षरों में कैद बहस
रोहित धनकर
नई शिक्षा नीति के निर्माण में आम जन की भागीदारी स्वागतयोग्य है, मगर ट्विटर
मार्का बहस सुसंगत निष्कर्षों तक नहीं पहुंचा सकती.
अप्रैल के महीने में मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने नई
शिक्षा नीति के निर्माण के लिए आम जनता को आमंत्रित करने के फैसले की जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि सरकार ने mygov वेबसाइट के जरिये "पहली बार आम नागरिक को
नीतिनिर्माण के काम में हिस्सेदार बनाने का प्रयास किया है, जो अब तक चंद लोगों तक
सीमित था." सरकार के इस कदम की सराहना की जानी चाहिए क्योंकि एक लोकतंत्र के
भीतर नीतिनिर्माण में लोगों की ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी से ही बेहतर नीतियां
बनती हैं. कम से कम सिद्धांत रूप में यह बात सही है.
लेकिन वेबसाइट
मेंलोगों की टिप्पणियों को 500 अक्षरों और चंद पूर्वनिर्धारित मुद्दोंतक सीमित कर
दिया गया है. इस तरह आंशिक रूप से सेंसर की गयी रायशुमारी से ज्यादा से ज्यादा
विखंडित और विरोधाभासी सुझाव ही जनता की ओर से मिल पाएंगे. हालांकि विरोधाभासी
दृष्टिकोण स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान हैं, फिर भी उन्हें तर्कपूर्ण व व्यवस्थित किए
जाने की जरूरत पड़ती है. दूसरे शब्दों में- अगर उन्हें शिक्षा पर एक व्यापक आधार
वाले संवाद के उद्देश्य से एकत्र किया जा रहा है तो उन्हें सुविचारित तर्कके रूप
में प्रकट करना होगा.
दूसरे, महत्वपूर्ण दलीलें 500
अक्षरों के अतिसूक्ष्म दायरे में व्यक्त नहीं की जा सकतीं. 500 शब्दों की सीमा के
बारे में कहा जा सकता है कि वेबसाइट पर फाइल अपलोड करने की भी छूट है, पर इस तरह
अपलोड की गई फाइलें बहस का हिस्सा नहीं बन पातीं. इस तथ्य को वेबसाइट में मौजूद
टिप्पणियों को देखकर भी समझा जा सकता है. इसलिए, यह निष्कर्ष निकालना गलत नहीं होगा
कि जनता के विचारों को जानने का यह तरीका स्वयं विचारों के विखंडन का पक्षपोषण
करता है.
विखंडित विवेक का दौर
मगर यह विखंडित विवेक का दौर है. समाज को इस मान्यता की ओर
धकेला जा रहा है कि चिंतन का मतलब विचारों को टुकड़ों में यहां-वहां उछालना भर होता
है. वैसे ही जैसे लोग ट्विटर में विचारों को उछालते रहते हैं. विचारों के ये टुकड़े
दरअसल किसी खास सन्दर्भ में ही अर्थपूर्ण होते हैं. इस किस्म के विखंडित विचारों
से निर्मित संवाद केवल अधपके तर्कों को ही तैयार करता है. वर्तमान सरकार द्वारा कराए
जा रहे नीति सम्बन्धी विचार-विमर्श, चाहे इनकी पद्धति की वजह से कहें या फिर समझ
की कमी के कारण,महज विचारों के विखंडित और अस्पष्ट बादलों के सामान हैं. यह ट्विटर
युग का विवेक है.
हमारी संस्कृति
और राज-व्यवस्था की एक सामान्य प्रासंगिक पृष्ठभूमि कहीं नज़र नहीं आती. यह मान
लेगा गलत होगा कि हम अपनी सांस्कृतिक, सामजिक, राजनीतिक और आर्थिक ज़रूरतों को एक
सा ही समझते/देखते हैं. ट्वीट करने की थोड़ी-बहुत सार्थकता हो सकती है लेकिन कुल
मिलाकर यह एक आधी-अधूरी राय ही है. इससे विचारों के आदान-प्रदान का भ्रम पैदा होता
है मगर विचार करने वाले के वास्तविक तर्क और इरादे छुपे रह जाते हैं. शिक्षा जैसे
महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक सुसंगत तर्क और व्यापक सहमति बनाने के लिए सन्दर्भ बताना
बेहद ज़रूरी है.
ऑक्सफोर्ड
डिक्शनरी के अनुसार नीति (पॉलिसी) एक तरह की दिशा या कार्य को निदेशित करने का
सिद्धांत है जिसे किसी संगठन या व्यक्ति ने अपनाया अथवा प्रस्तावित किया हो. इसे
विशिष्ट गतिविधियों या क्रियाओं को पैदा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है. इसे
किन्हीं खास सुझाओं और सिफारिशों की स्वीकार्यता को जांचने के लिए इस्तेमाल किया
जाता है.
मानव संसाधन मंत्रालय इसके द्वारा
नियोजित सिलसिलेवार बहस-मुबाहिसे से शिक्षानीति की ऐसी ही रूपरेखा की उम्मीद कर
रहा है. mygov वेबसाइट के मुताबिक मंत्रालय ने वेबसाइट पर जो समूह बनाया है उसका उद्देश्य
"समावेशी, सहभागितापूर्ण और समग्र दृष्टिकोण से देश के लिए एक नई शिक्षा नीति
तैयार करना है." वेबसाइट पर 'संवाद' आयोजित करने के अलावा मंत्रालय की एक
"पूर्व परिभाषित सर्वेक्षण प्रश्नावली" के माध्यम से राष्ट्रव्यापी
परामर्श एकत्र करने की भी योजना है. इसके लिए भी एक समूह का गठन हो चुका है, एक सरकारी
अधिकारी की अध्यक्षता में, हालांकि यह अब तक रहस्यों में घिरा है- जिस जनता से नई
नीति पर अपनी राय बताने की अपेक्षा की जा रही है, उसे भी इसके सदस्यों के बारे में
कोई जानकारी नहीं है.
दोषपूर्ण पद्धति
इस प्रकार शिक्षा नीति तैयार करने की पद्धति में कम से कम
दो गंभीर समस्याएं हैं. पहली, ट्विटर मार्का विचारों की सही-सही व्याख्या की दरकार
होती है. लेकिन यह व्याख्या उसी रहस्यमय समूह के हवाले कर दी गई है, जो एक सरकारी
अधिकारी की अध्यक्षता में बनाया गया है. व्याख्या के लिए एक सामान्य वैचारिक
रूपरेखा की जरूरत पड़ती है, जिसके बारे में चुप्पी साध ली गयी है या उसे सार्वजनिक
नहीं किया गया है. इसलिए व्यक्त किए गए विचार पहले से तयशुदा नीतियों को पुष्ट
करने के इरादे से तोड़े-मरोड़े जा सकते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि एक छोटे से पसंदीदा
समूह के पूर्व-निर्धारित निर्णयों को एक अप्रभावी जन-संवाद के जरिये सही ठहराया जा
सकता है.
दूसरी, सर्वानुमति
बनाने के किसी आधारभूत निर्देशक सिद्धांतों के अभाव में इस कवायद का वही नतीजा
निकलेगा जिसे शिक्षा के जाने-माने दार्शनिक जॉन व्हाइल "एचसीएफ समस्या"
कहते हैं. समूची कवायद से ऐसे अस्पष्ट और अपुष्ट सुझावों का ढेर लग जाएगा, जिनके
बीच सामाजिक न्याय और समता के मुद्दे गायब होंगे- क्योंकि इस तरह भिड़ाए गए इन
मुद्दों पर कोई आसान सी सहमति उपलब्ध नहीं है. और इस तरह समाज की वास्तविक चिंताएं
या तो महत्वहीन हो जाएंगी या सिरे से नदारद होंगी.
इस
विचार-विमर्श के प्रयोजन और उद्देश्य को समझने के लिहाज से प्राथमिक शिक्षा के लिए
चुने गए 13 प्रकरणों का पाठ बड़ा दिलचस्प है. प्रत्येक प्रकरण का करीब 200 शब्दों
में परिचय दिया गया है और साथ में विमर्श के लिए सवालों की एक सूची है. ज्यादातर
सवाल इसके संचालन की बारीकियों से जुड़े हैं. नीति से इनका कोई खास संबंध नहीं है.
उदाहरण के लिए,
एक सवाल में यह पूछा गया है कि टेक्नोलॉजी का शिक्षकों की वास्तविक मौजूदगी को
सुनिश्चित करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है. सवाल के गठन से ही स्पष्ट
हो जाता है कि मुद्दा यह नहीं कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं, बल्कि
यह है कि कैसे इसे इस्तेमाल करना चाहिए. अगर सवाल 'क्या' से शुरू होता तो यह
शिक्षक की विश्वसनीयता, स्वायत्तता, जिम्मेदारी व सम्मान जैसे सभी महत्वपूर्ण
मुद्दे उठाता. लेकिन 'कैसे' जोड़ देने से यह पहलेही तय हो गया कि शिक्षकों की कड़ाई
से निगरानी करनी चाहिए और उन्हें दंड का भय दिखाना चाहिए. इसलिए 'क्या टेक्नोलॉजी
का इस्तेमाल करना चाहिए' जैसा सवाल एक नीति से जुड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि यह
सामान्य सिद्धांतों के गिर्द घूमता है, जबकि 'कैसे' जुड़ने वाली चर्चा एक तकनीकी
सवाल है जिसका नीति से कोई खास ताल्लुक नहीं बल्कि यह कार्यान्वयन का मसला है.वेबसाइट
में ज्यादातर प्रश्न इसी मिजाज़ के हैं.
यहां ध्यान
देने लायक बात यह है कि प्रकरणों के परिचय में ही कई पूर्व निर्धारित नीतियां छुपी
हुई हैं. उदाहरण के लिए, स्कूल स्तर पर परीक्षा सुधार वाला प्रकरण कहता है कि
"परीक्षा सुधार शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को बदल देगा और अधिगम परिणामों में
सुधार लाएगा." यह विचार के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता था कि क्या
'परीक्षा-उन्मुख सुधार' सफल हो सकते हैं, अथवा वे 'परीक्षा के लिए पढ़ाई' को
प्रोत्साहन देंगे और इस तरह समालोचनात्मक तार्किकता के लिए दी जाने वाली शिक्षा का
ही बंटाधार कर डालेंगे. परीक्षा का डर क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी
समस्याओं में एक नहीं है? लेकिन यहां, परीक्षा-उन्मुख सुधार को आस्था के एक तत्व
की तरह स्वीकार कर लिया गया है.
मैं शिक्षा
नीति पर सार्वजनिक बहस की मुखालिफत नहीं कर रहा हूं. न ही मैं शिक्षा से जुड़े
महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किए जाने के विरोध में हूं. एक लोकतांत्रिक देश में
शिक्षा नीति पर फैसले लेने के लिए ये दोनों सामान रूप से आवश्यक हैं. दिक्कत सिर्फ
इतनी है कि तयशुदा सवालों और पूर्व-निर्धारित प्रकरणों से गहरे और निष्पक्ष
वाद-विवाद की संभावना सीमित हो जाती है.
आज भारतीय
शिक्षा तीन दिशाओं से खिंचाव महसूस कर रही है. पहली दिशा, शिक्षा को आर्थिक वृद्धि
की जरूरतों के अनुरूप ढालने की वकालत की है. इसमें व्यावहारिक कौशल-निर्माण और
पर्याप्त कार्यशक्ति तैयार करने पर जोर दिया जाता है. दूसरी दिशा शिक्षा को
लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को हासिल करने की ओर ले जाने की है. इसमें समाज,
राजनीति, अर्थतंत्र की आलोचनात्मक समझ बनाने तथा ज्यादा समतामूलक व सामंजस्यपूर्ण
समाज के लिए मूल्यों का ढांचा गढ़ने पर जोर दिया जाता है. तीसरी दिशा, जो दिन पर
दिन मजबूत होती जा रही है, शिक्षा को भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के एक खास नजरिये
से जोड़ने का दबाव बनाती है. इसका जोर पाठ्यक्रम में हिन्दू नायकों, ग्रंथों और
आचरण के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह बनाने पर है. तीनों तरह के खिंचाव समाज और
राज्य-व्यवस्था की जरूरतों के अलग-अलग दृष्टिकोणों को रेखांकित करते हैं. उदाहरण
के लिए, पहला आर्थिक खिंचाव जहां बिकाऊ कौशलों पर जोर देता है, वहीं राजनीतिक
आलोचना और सामाजिक न्याय के मुद्दों की उपेक्षा करता है. इसका परिणाम एक कार्यक्षम
किन्तु दब्बू कार्यशक्ति और उपभोक्तावाद के विस्तार के रूप में प्रकट होगा. दूसरी
ओर, एकमात्र सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा को समर्पित कर देने का परिणाम वही होगा
जिसे कोठारी आयोग की रिपोर्ट "बेरोजगार स्नातकों की फ़ौज”
कहती है. जो सामाजिक न्याय हासिल करने में भी नाकामयाब होगी. और भारतीय संस्कृति व
इतिहास की इकतरफा समझ पर जोर देने का परिणाम समाज में विभाजन और कडुआहट के
बीजारोपण के रूप में प्रकट होगा. जो आर्थिक प्रगति के साथ-साथ लोकतंत्र तथा सामाजिक
न्याय को भी नष्ट कर डालेगा.
सरकार का
ट्विटर मार्का बहस-मुबाहिसे पर जोर यह बताता है कि वह किसी दीर्धकालिक संवाद के
पक्ष में नहीं है. पूर्व परिभाषित बिंदुओं और तयशुदा सवालों के जरिए संकीर्ण दायरे
में सार्वजानिक बहस को खोलने की रणनीति वास्तविक नीतिगत मुद्दों पर बहस को पहले ही
रोक देती है. इस तरह निर्णय कुछ चुनिन्दा हाथों तक सिमट जाते हैं. खुली लोकतांत्रिक
बहस का भ्रम पैदा किया गया है लेकिन असल में जनता का दिमाग छोटे-छोटे मामूली
विवरणों में उलझाया जा रहा है.
(रोहित धनकर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, बंगलुरु में अकादमिक विकास विभाग के
प्रोफ़ेसर व निदेशक हैं.
साथ ही वह दिगंतर, जयपुर के अकादमिक सलाहकार भी हैं.)