 आधुनिक भारत में पारसी थियेटर जो प्रकारांतर से हिन्दी सिनेमा की नींव भी बना, के अन्यतम अभिनेता-निर्देशक और बहुआयामी व्यक्तित्व के इन्सान मास्टर फिदा हुसैन के बारे में महामहोपाध्याय अशोक पांडे ने कुछ दिनों पहले कबाड़खाना पर परिचयात्मक पोस्ट लगाई थी जिसे देखकर याद आया कि हमारे ख़ज़ाने में भी मास्टरजी पर कुछ दुर्लभ सामग्री है। हमने यूं भी उसे कबाड़खाना पर ही सजाने का सोचा था, पांडे जी का आदेश था कि यह काम जल्द अज़ जल्द हो जाए। शब्दों का सफ़र से फुर्सत कम ही मिलती है...फिर भी साझेदारी के सुख से न हम महरूम रहना चाहते हैं और हमसफरियों और कबाड़ियों को रखना चाहते हैं।
आधुनिक भारत में पारसी थियेटर जो प्रकारांतर से हिन्दी सिनेमा की नींव भी बना, के अन्यतम अभिनेता-निर्देशक और बहुआयामी व्यक्तित्व के इन्सान मास्टर फिदा हुसैन के बारे में महामहोपाध्याय अशोक पांडे ने कुछ दिनों पहले कबाड़खाना पर परिचयात्मक पोस्ट लगाई थी जिसे देखकर याद आया कि हमारे ख़ज़ाने में भी मास्टरजी पर कुछ दुर्लभ सामग्री है। हमने यूं भी उसे कबाड़खाना पर ही सजाने का सोचा था, पांडे जी का आदेश था कि यह काम जल्द अज़ जल्द हो जाए। शब्दों का सफ़र से फुर्सत कम ही मिलती है...फिर भी साझेदारी के सुख से न हम महरूम रहना चाहते हैं और हमसफरियों और कबाड़ियों को रखना चाहते हैं।
पेश है इस श्रंखला की पहली किस्त। हिन्दी रंगमंच की दुनिया का जाना माना नाम है प्रतिभा अग्रवाल का। कोलकाता के श्यामानंद जालान के साथ मिलकर भारतीय रंगमंच के लिए ऐतिहासिक महत्व का काम किया है। प्रतिभाजी ने 1978 से 1981 के दरम्यान मास्टरजी के साथ लगातार कई बैठकें कर उनके अतीत की यात्रा की। मास्टरजी के स्वगत कथन और बीच बीच में प्रतिभाजी के नरेशन की मिलीजुली प्रस्तुति बनी एक किताब जो मास्टरजी के जीवन के बारे में और इस बहाने पारसी रंगमंच की परम्परा और नाट्य परिदृश्य की जानकारी देनेवाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यहां इस पुस्तक के चुने हुए दिलचस्प अंश प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
दिल्ली से लौटने वाले मुरादाबाद भी पहुंचे और एक दिन इनके मुहल्ले में ही कठपुतली का खेल हुआ। खाट खड़ी करके, चादर बांध कर खेल दिखाया गया। कहानी थी किसी बादशाह की। बादशाह था, उसका वजीर था, सिपहसालार था, सेनापति था। कुछ कहासुनी हुई, एक दूसरे से झगड़ा हुआ और तलवारबाजी हुई। अच्छा लगा। खेल में कहानी थी और वह मन पर ऐसी छा गई कि घर आकर वही हरकतें शुरू कर दीं। कहने का मतलब यह कि नाटक और एक्टिंग की शुरुआत यहीं से हुई। खैर, यह किस्सा तो आया गया खत्म हो गया पर गाने का शौक बना रहा। रोज कहीं न कहीं सुनने पहुंच जाते और घर में पता लगने पर पिटाई होती। मां का तब तक स्वर्गवास हो चुका था, पर पिता थे, बड़े भाई थे। सबसे बड़े भाई की शादी भी हो चुकी थी। एक बार जब वे फिदा हुसैन की हरकतों से तंग आ गए तो उन्होंने बीवी के हाथों इन्हें पान में सिंदूर दिलवा दिया ताकि आवाज बंद हो जाए। वह किस्सा फिदा हुसैन साहब की जुबानी सुनिए।

``जब मैनें गाने का शौक नहीं छोड़ा तो तंग आकर भाई साहब ने भाभी के जो मुझे बहुत प्यार करती थीं, उनके हाथों से मुझे पान में सिंदूर दिलवा दिया कि आवाज ही खत्म हो जाए। और लोग भी एतराज करते थे। तो मेरी आवाज बंद हो गई। करीब चार-पांच महीने तक मेरी ये हालत रही कि मैं सांय-सांय बोलता, सर पटकता था। मगर आवाज ही नहीं। और दवाईयां जितनी कर सकता था की। लेकिन कुछ हुआ नहीं, पर लगन मेरी थी। मैं एकांत में रोता था और ईश्वर से प्रार्थना करता था कि मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, बस मेरा सुर ठीक हो जाए। पर वह ठीक ही न हो। कुछ रोज के बाद जन्माष्टमी पड़ी। हमारे मुरादाबाद में किला का मंदिर है। वहां जन्माष्टमी के समय मंडलियां आती हैं, संत लोग आते हैं। तो वहां एक संत आए हुए थे। उनकी बड़ी हस्ती थी।
मैं इस तलाश में रहता था कि कोई मिले, मुझे कोई उपाय बता दे। मतलब बड़ी बुरी हालत थी। तो में वहां पहुंच गया। चौरासी घंटा मुहल्ला है मेरे मुहल्ले के पीछे ही, वहीं पहुंच गया। देखा, धूप में चबूतरे के ऊपर एक विशाल मूर्ति , बहुत सफेद दाढ़ी। वे तकिया लगाकर चारपाई पर बैठे थे और एक आदमी उनका पैर दबा रहा था। वहां बल्लम का पहरा था, भाला लेकर संतरी खड़ा था। मैं अंदर दरवाजे में जाने लगा तो उन लोगों ने रोक दिया और मैं परेशान कि क्या करुं । फासला था फिर भी उनकी नजर मुझ पर पड़ गई। उन्होंने कहा `आने दो, आने दो। मतलब ये कि जानते हुए भी कि मुसलमान है, इसीलिए इसको रोक रहे हैं, उनके मुंह से निकला `आने दो, आने दो। मैं पास आ गया। आने के साथ उनके पैर पकड़कर, पैर फैला था इतना, रोने लगा। और लोगों ने कहा कि , `ठहरों इसे अलग करों तो उन्होंने कहा `नहीं, रो लेने दो, इसका मन हलका हो जाने दो।
मैं दो-तीन मिनट तक रोता रहा। उसके बाद एक शेख खड़े थे वहां पे, उन्होंने कहा- साहब का कंठ खराब हो गया है। इसका कंठ बहुत अच्छा था। भजन-वजन में भी कभी-कभी आता था ये। तो बोले अच्छा । पास बुलाया, बोले-`कैसे हुआ। सब बता दिया तो बाले- `अच्छा दवा तो मैं खास कोई नहीं बताऊगा। एक साधना बताता हूं और संभव है कि उससे तुमको फायदा पहुंचे, लाभ मिल जाए। दवा में सिर्फ ये है कि जिसने तुमको सिंदूर दिया है (भाभी ने) उसके ही हाथ से पक्का केला घी में तलवाकर तीन रोज तक खाओ। और साधना यह कि कुएं के ऊपर लेटकर, गर्दन कुएं में लटका कर जब तक तुम्हारा सुर साफ न हो जाए सुर भरो, आ-आ करते रहो। मैं लौट आया। मकान के बाहर कुआ था। वहां तो मैं ये कर नहीं सकता था। पास ही एक जगह थी जहां कोई नहीं जाता था। पास ही एक जगह थी, जहां कोई नहीं जाता था। वहां दसमा घाट है। वहां के लिए मशहूर था कि खजूर पर कोई भूत रहता है। लेकिन मैं तो भूत-वूत को नहीं मानता था। मैं दोपहरी में वहां पहुंच जाता। एकांत रहता। कुएं पर लेटकर आ-आ करता। कोई 10-20 रोज तक यह करता रहा, पर कोई फायदा नहीं पहुचा। केले की दवा भी कर ली थी लेकिन कुछ हुआ नहीं। पर मैं हिम्मत नहीं हारा। उन्होंने कहा था जब तक न हो करते रहना। मुझे उनका कहना याल में था। कोई 20 रोज के बाद 21 दिन मुझे मालूम हुआ कि आवाज कुछ शुरू हुई। 26 दिन के अंदर्र-अंदर मेरा गला साफ हो गया। जैसा सुर वैसा फिर हो गया। जारी
ऊपर का चित्र कश्मीर हमारा है नाटक का।
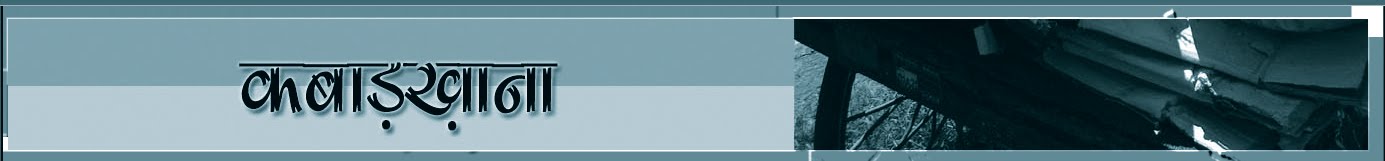




 काम से आराम
काम से आराम

















