सुन्दर
सुरुक्कई बंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ़ एडवांस्ड स्टडीज में प्रोफेसर हैं. उनके
इस महत्वपूर्ण लेख का अनुवाद कबाड़खाने के लिए प्रिय मित्र आशुतोष उपाध्याय ने किया है.
नई टेक्नोलॉजी और
पुराना धर्म
- सुन्दर
सरुक्कई
संवर्धित यथार्थ हमारे
ब्रह्माण्ड को नया रूप देने के लिए
भौतिक संसार व मनुष्य की
लालसा के बीच सेतु को उलट रहा है.
आकाशवाणी हो चुकी है. उनका सपना जल्द ही आपके निजी गैजेट
का रूप धर लेगा. एफ 8 की पिछले माह संपन्न सालाना ग्लोबल डेवेलपमेंट कांफ्रेंस में
फेसबुक के सीईओ मार्क ज़ुकरबर्ग ने नई टेक्नोलॉजी के बारे में अपनी परिकल्पनाओं का
खुलासा किया. वह हमारी ज़िंदगियों को बदल डालना चाहते हैं. इसके लिए वह उन
तौर-तरीकों को बदलना चाहते हैं, जिनके जरिये हम अपने आस-पास की वास्तविक दुनिया को
महसूस करते, उससे जुड़ते और उसका अनुभव करते हैं. वह हमारी रोजमर्रा दुनिया के ठोस
यथार्थ को मसालेदार संवर्धित यथार्थ (अगमेंटेड रियलिटी) में बदलना चाहते हैं. मसलन,
एक ऐप के ज़रिए वह हमारे दलिये के कटोरे को तैरती हुई छोटी-छोटी शार्कों की छवियों
से भर सकते हैं.
संवर्धित
यथार्थ कुछ इसी तरह का है. यह हमारे सामने पसरी दुनिया से उपजने वाली असंतुष्टि की
ज़मीन पर उगना शुरू करता है. यह हमारी निकृष्टतम लालसाओं को पंख लगाता है. इसके लिए
एक ऐसी दुनिया का सृजन करता है जो हममें से हरेक के लिए ख़ास होती है, मानो हमारी
इच्छाओं की ग़ुलाम हो जबकि हकीक़त इससे ठीक उलट होती है.
जाना-पहचाना प्रलोभन
ज़ुकरबर्ग के सपने में कुछ भी नया नहीं है. हालांकि इसे कुछ
इस तरह परोसा गया मानो निहायत नयी चीज़ हो. लेकिन टेक्नोलॉजी की इस नई परिकल्पना
में बहुत कुछ वही है जो कभी प्राचीन धार्मिक कल्पनाओं का हिस्सा रहा है.
ज़ुकरबर्ग चाहते हैं कि हम "अपने आसपास की उन तमाम
चीज़ों के बारे में सोचें जिन्हें वास्तव में भौतिक स्वरूप की ज़रूरत नहीं है."
दुनिया के पदार्थ रूप पर संदेह करने वाला उनका सपना ऐसे तकनीकी प्रयास की ओर इशारा
करता है जो हमेशा सामने मौजूद वास्तविक यथार्थ के पार जाता है. नई टेक्नोलॉजी का
यह नजरिया पुरानी धार्मिक कल्पनाओं से काफी-कुछ मेल खाता है. यह कहता है कि हम
जितना डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल होते जाएंगे, हमारी धार्मिकता उतनी ही सघन होती
जाएगी. क्या इसे सिर्फ संयोग माना जाय कि इस डिजिटल युग के साथ धार्मिकता और
नव-गुरुओं की संख्या में ज़बरदस्त इजाफ़ा हुआ है?
अगर यह बात आपको बेतुकी लगे तो कृपया इस विश्लेषण पर गौर
करें. धर्म की तरह यह नई टेक्नोलॉजी भी वास्तविक भौतिक दुनिया पर संदेह से शुरू
होती है. यह हमेशा उससे ज्यादा की मांग करती है जो हमारे सामने ठोस रूप में मौजूद
है. टेक्नोलॉजी और धर्म दोनों भौतिक शरीर को नश्वर जगत की तमाम समस्याओं की धुरी
मानते हैं. भौतिक दुनिया के मकड़जाल से भाग निकलने के लिए वे मुक्ति व स्वतंत्रता
के चुनिंदा विचारों का इस्तेमाल करते हैं.
टेक्नोलॉजी और धर्म दोनों मनुष्य के कर्म की स्वायत्तता की
बुनियाद पर ही सवाल खड़े करते हैं: क्या हम ईश्वर के सम्मुख अपनी स्वायत्तता को ठीक
उसी तरह नहीं खो बैठते जैसे हम डिजिटल गैजेटों के सामने खो देते हैं? दोनों चमत्कार
का इस्तेमाल करते हैं और अपनी ओर खींचने के लिए हमारी आँखों पर अपने रंग का चश्मा
चढ़ा देते हैं. दोनों सुरक्षा और आश्वस्ति का अहसास देते हैं और अपने प्रति एक तरह
की निर्भरता पैदा करते हैं. और अंत में उस एक जैसी रणनीति को नहीं भूलना चाहिए जो
ये दोनों इस्तेमाल करते हैं: कीमत का सवाल.
धर्म
बहुत सस्ते में हमें तमाम सुविधाओं का वादा करता है. ज़ुकरबर्ग ने भी यह पाठ अच्छी
तरह सीखा है: वह अपना सपना इस दावे के साथ बेचते हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से भविष्य
में 500 डॉलर के एक टीवी का काम 1 डॉलर का ऐप कर डालेगा. लेकिन भौतिक संसार के साथ
वास्तव में समस्या क्या है? आखिर डिजिटल टेक्नोलॉजी वालों और धार्मिक कल्पनाकारों
को भौतिक वास्तविकता का विचार इतना दिक्कततलब क्यों लगता है?
मानवीय और दैवीय
इंसानों की दुनिया और दैवीय संसार के बीच फ़ासला बहुत बड़ा
है. इस फ़ासले के एक पक्ष को इंसानों के भौतिक अस्तित्व से परिभाषित किया जा सकता
है. हम सब हाड़-मांस के बने हैं, जगह घेरते हैं और भौतिक उत्पादों पर जीवित रहते
हैं. हमारा शरीर भौतिकता की जीती-जागती मिसाल है और यही शरीर मुक्ति की कई
अवधारणाओं के लिए भी मुसीबत बन जाता है.
शरीर एक समस्या है क्योंकि कोई भी भौतिक वस्तु, परिभाषानुसार,
नियमों के दायरे में संचालित होती है. शरीर इस लिहाज से भी एक भौतिक निकाय है क्योंकि
अपनी भौतिकता के कारण यह कई चीज़ें नहीं कर पाता. मुक्ति का विचार प्रथमतः भौतिक
दुनिया से मुक्ति की बात करता है. देवलोक भौतिक दुनिया को परिभाषित करने वाले
कारकों से संचालित नहीं होता. ईश्वर और फ़रिश्ते उड़ सकते हैं लेकिन हम नहीं. वे समय
और काल की सीमाओं से भी बंधे हुए नहीं हैं. ईश्वर हमारी तरह नहीं होते. परिभाषा के
मुताबिक़ वे अपदार्थ हैं, सर्वत्र हैं, अविनाशी हैं, आत्मा हैं, चेतना हैं. ईश्वर
डिजिटल दुनिया का पहला उदाहरण है जिसे भौतिक शरीर जैसी कोई बाधा नहीं बांधती. पश्चिम
की परम्परा में ईश्वर के विचार की गणित के साथ गहरी साम्यता की यह भी एक वजह है.
ज्यामिति को ईश्वर की सर्वत्रता, जबकि अंकगणित को उसकी निरंतरता का प्रतिरूप माना
जाता है. आइजैक न्यूटन उन विद्वानों में गिने जाते हैं जिन्होंने इन दो अभौतिक
क्षेत्रों के बुनियादी सम्बन्ध को स्वीकार किया था.
संवर्धित यथार्थ इस चीज़ को एक कदम और आगे ले जाता है. यह
विज्ञान और टेक्नोलॉजी की कल्पनाशक्ति का तार्किक अंत है. विज्ञान दुनिया की अपने
ढंग से विवेचना करता है लेकिन विज्ञान का लक्ष्य मात्र विवेचना तक सीमित नहीं
रहता.
विज्ञान का बुनियादी उद्देश्य इस विवेचना को इस्तेमाल करना
और उस दुनिया के साथ कुछ न कुछ करना है, जिसकी यह विवेचना करता है. विज्ञान अमूमन
प्रकृति के ज्ञान को इस्तेमाल करता है ताकि इसे नियंत्रित व काम में लाया जा सके.
यद्यपि, विज्ञान का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है: आखिरकार प्रकृति की रचना करना.
विज्ञान के लिए यह जान लेना पर्याप्त नहीं कि चीज़ें जैसी
दिखाई देती हैं वैसी क्यों हैं या वे क्यों इस तरह व्यवहार करती हैं. उसके लिए इससे
भी ज्यादा ज़रूरी है कि कैसे इस दुनिया को रचा जाय, बल्कि और 'बेहतर' कैसे रचा जाय.
विज्ञान का अंतिम लक्ष्य दरअसल ईश्वर बन जाना है, क्लोनिंग, बीटी फसलें, कृत्रिम
बुद्धि और संवर्धित यथार्थ इस यात्रा की शुरुआत के डगमगाते कदम भर हैं.
धर्म और ज़ुकरबर्ग में एक और बात समान है. दोनों इस तथ्य पर
निर्भर हैं कि मनुष्य खुद से और इस दुनिया से हमेशा नाराज़ रहते हैं. धर्म उन्हें
दूसरे लोक की, परलोक की घुट्टी पिलाकर तसल्ली देता है. ज़ुकरबर्ग अपने डिजिटल
खिलौनों में एक स्वर्ग रचना करना चाहते हैं. वह हमें खुद को बदलने सलाह देने के
बजाय हमारी दुनिया को ही बदल देना चाहते हैं.
ईश्वर
का दायरा हम इंसानों की दुनिया से अलग है. इसलिए मुक्ति का मतलब इस जगह को छोड़कर
इसके परे कहीं और जाना बताया जाता है. मगर संवर्धित यथार्थ इस किस्म की मुक्ति की
बात नहीं करता. यह हममें हरेक के दरवाजे के बाहर एक स्वर्ग की रचना करना चाहता है.
या कम से कम हममें से हरेक के स्मार्टफोन के बाहर.
सामाजिक साझेदारी की मनाही
सामान्यतया धर्म के विपरीत संवर्धित यथार्थ आत्ममुग्धता से
परिपूर्ण और आत्म-केन्द्रित होता है. धर्म हमेशा से सामाजिक रहे हैं. वे सामाजिक
रूप से व्यवहार में लाये जाते हैं और सामाजिक कर्मकांडों से भरे होते हैं. लेकिन
इस नए तकनीकी कृत्रिम संसार में, जिसे हममें से हरेक अपनी लालसाओं व फंतासियों के
अनुरूप गढ़ सकता है, सामाजिक साझेदारी की गुंजाइश नहीं है. यह एक व्यक्ति को रचता
है और बाहरी संसर्ग से अलग करता है, जिसका अंत सामाजिक मतिभ्रमता में होता है.
यह डिजिटल दुनिया है, क्षणभंगुर, अनिर्धारित, स्वतंत्र और
चलायमान प्रतीत होती, जो इंसान के हकीकी दुनिया से बाहर का रास्ता दिखाती है. यह
नई टेक्नोलॉजी एक नए धर्म का मायाजाल रचने के लिए वह सब देने का स्वांग भरती है,
जिसे देने की बात पुराना धर्म करता था. तमाम धर्मों की तरह यह भी भूल जाती है कि
डिजिटल और क्षणभंगुर हमेशा पदार्थ की बुनियाद पर ही खड़े हैं. ठीक उसी तरह जिस
प्रकार मनुष्य जीवन निरंतर खोते जाने और मौत की आधारशिला पर खड़ा है.
ज़ुकरबर्ग हमें केवल बाहरी चकाचौंध के दर्शन करा रहे हैं. इसे
हकीकत में बदलने वाले पीछे रखे तारों और ब्लैक बॉक्सों को वह नहीं दिखाते. लेकिन
आखिरकार वह उन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं, जिन्हें उन्होंने सिरजा है. ये हम
हैं, पीड़ित, बोझ से दबे सशरीर इंसान,जो उनके पास अपनी लालसाओं की क्षुधा शांत करने
के लिए जाते हैं. हम अपने डिजिटल मालिकों के हाथों की कठपुतलियां हैं. और हम उस
बिंदु से आगे निकल आए हैं कि पूछ सकें कि क्या हम अपनी कारगुजारियों और मंजिल को
जानते हैं. हम इस नए धर्म की ज़मीन में पांव रख चुके हैं.
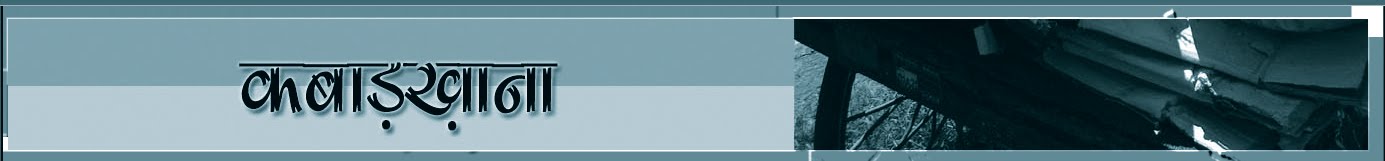

No comments:
Post a Comment